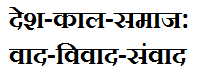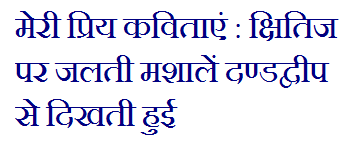-कविता कृष्णपल्लवी
(फेसबुक पर डाले गये राहुल सांकृत्यायन के उद्धरण पर सुरेश काण्टक ने एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के जवाब में यह टिप्पणी लिखी गयी है।ज्यादा साथियों तक पहुँचाने के लिए इसे ब्लॉग पर दे रही हूँ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
अपने प्राचीन काल के गर्व के कारण हम अपने भूत के स्नेह में कड़ाई के साथ बँध जाते हैं और इससे हमें उत्तेजना मिलती है कि अपने पूर्वजों की धार्मिक बातों को आँख मूँदकर मानने के लिए तैयार हो जाएं। बारूद और उड़नखटोला में तो झूठ-साँच पकड़ने की गुंजाइश है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में तो अँधेरे में काली बिल्ली देखने के लिए हरेक आदमी स्वतंत्र है। न यहाँ सोलहों आना बत्तीसों रत्ती ठीक-ठीक तोलने के लिए कोई तुला है और न झूठ-साँच की कोई पक्की कसौटी।
-राहुल सांकृत्यायन
धर्म वह मानव निर्मित नियमावली है जिसका सम्बंध तत्कालीन समस्याओ के समाधान से होता है , इसे रूढ् नहीँ विकाशमान स्थितियो मेँ समझना होगा । हर युग का धर्म परिवर्तनशील है ,पूर्व निर्धारित नहीँ ।
-सुरेश काण्टक
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
धर्म एक सुनिश्चित ऐतिहासिक प्रवर्ग है, जिसकी हम मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते । एक मानवेतर सत्ता द्वारा हमारी नियति तय किया जाना या हमारे कर्मफलों पर न्याय-निर्णय दिया जाना और नैतिकता के नियमों का निर्धारण किया जाना, एक पारलौकिक जगत का अस्तित्व में होना, आत्मा का गमनागमन आदि -- ये धार्मिक विश्वदृष्टिकोण के मूल तत्व हैं। धार्मिक विश्वदृष्टिकोण के पहले प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, 'प्रोटो-टाइप'धर्म या जादुई विश्वदृष्टिकोण का कालखण्ड था। निश्चय ही उन युगों में पिछड़े हुए मनुष्य को अज्ञात प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध टिके रहने में, तथा आगे चलकर सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ने में भी धर्म ने मदद की थी। पर उसकी मुख्य भूमिका राजा की सत्ता को मानवेतर स्वीकृति प्रदान करने की ही थी। धर्म पिछड़ी, अवैज्ञानिक चेतना में सामाजिक यथार्थ के परावर्तन का ही एक रूप था। पुनर्जागरण के साथ 'थियोसेण्ट्रिक सोसाइटी''एन्थ्रोपोसेण्ट्रिक सोसाइटी'बनी, प्रबोधन काल ने वैज्ञानिक तर्कणा के धरातल को और ऊँचा किया और धार्मिक विश्वदृष्टिकोण के बरक्स वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण स्थापित हुआ। फिर भी आज समाज में धर्म और ईश्वर का अस्तित्व प्रभावी रूप में क़ायम है और आगे भी लम्बे समय तक बचा रहेगा। इसका मूल कारण है कि जीवन को चलाने वाली आज जो मूल ताक़त है -- माल-उत्पादन और पूँजी संचय की गतिकी -- वह आम आदमी के लिए अभी भी रहस्य है। इसी रहस्यात्मकता का परावर्तन ईश्वर की अदृश्य छवि में होता है। दूसरा कारण यह है कि सत्तासीन होने के बाद पूँजीपति वर्ग ने धर्म से ''पवित्र गठबंधन''कर लिया, उसे उत्पादन प्रक्रिया के लिए तो विज्ञान की ज़रूरत थी, पर जनता को नियतिवादी और निष्क्रिय बनाये रखने के लिए धर्म की ।
धर्म चाहे जितने नये-नये पैदा हों, उनकी मूल अन्तर्वस्तु वही रहेगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति और जीवन के सतत् बदलाव के साथ जीवन मूल्यों, नैतिक नियम-विधानों, सामाजिक-राजनीतिक ढाँचों के परिवर्तन की बात करता है। बेहतर है कि धर्म और विज्ञान की अवधारणाओं में पूर्वानुमानों के आधार पर घालमेल करने की जगह धर्म के इतिहास को नृतत्वशास्त्र और प्राचीन इतिहास के पुस्तकों से पढ़ा जाये, दिदरो, वाल्तेयर, टॉमस पेन के लेखन और धर्म विषयक मार्क्स-एंगेल्स और लेनिन की दार्शनिक विवेचनाओं को पढ़ा जाये और फिर एक धारणा बनायी जाये। धर्म ईश्वर निर्दिष्ट नियमों के नाम पर मानवनिर्मित नियमावली ही होती है, पर इसकी सार्विक स्वीकृति मध्ययुग तक ही थी। हालाँकि यह नियमावली बनाने वाले उससमय भी शासक वर्ग के हितों को ही ध्यान में रखकर बनाते थे(कुछ सत्ता विरोधी विद्रोही जन-धर्मान्दोलनों को छोड़कर)। आज भी धर्म ''मानवनिर्मित नियमावली''है, पर उसको बनाने वाले लोग और उनका विराट तंत्र पूँजी की सेवा में सन्नद्ध मानव हैं, समस्त मानव नहीं। मुक्तिकामी शोषित-उत्पीडि़तों जनों को विज्ञान का नेतृत्व चाहिए क्योंकि विज्ञान प्रकृति और समाज की गति का सामान्यीकरण करता हुआ उसे यह विश्वास दिलाता है कि सामाजिक बदलाव 'चांस'का खेल या महानायकों का चमत्कार नहीं है, उसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। धर्म का सार है -- रहस्यीकरण और अंधानुकरण। विज्ञान का सार है -- कारण-कार्य-सम्बन्धों की खोज द्वारा रहस्यभेदन और स्वतंत्र तार्किक विवेक द्वारा मार्ग चयन। विश्वसनीयता हासिल करने के लिए आधुनिक युग के धर्म कई बार विज्ञान का सहारा लेने का तर्काडम्बर करते हैं (जो विज्ञान के हाथों उसकी पराजय भी है), पर धर्म कभी विज्ञान नहीं हो सकता और वैज्ञानिक नियमों को कभी जड़-रूढ़ धर्मादेश नहीं बनाया जा सकता।