↧
'पहल' का मार्च अंक
↧
तकनोलॉजी और सामाजिक क्रम-विकास
यदि तकनोलॉजी का कोई आलोचनात्मक इतिहास लिखा जाये तो उससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि 18वीं सदी के किसी भी आविष्कार को किसी एक व्यक्ति का काम समझना कितना ग़लत है। अभी तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गयी है। डार्विन ने प्रकृति की तकनोलॉजी के इतिहास में, यानी पौधों और पशुओं की उन इन्द्रियों के निर्माण के इतिहास में, जो उनके भरण-पोषण के लिए उत्पादन के साधनों का काम करती हैं, हमारी रुचि पैदा कर दी है। तब क्या मनुष्य की उत्पादक इन्द्रियों का इतिहास - उन इन्द्रियों का विकास, जो समस्त सामाजिक संगठन का आधार है - इस योग्य नहीं है कि उसकी ओर भी हम उतना ही ध्यान दें? और क्या इसतरह का इतिहास तैयार करना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि विको ने कहा है, मानव इतिहास प्राकृतिक इतिहास से केवल इसी बात में भिन्न है कि उसका निर्माण हमने किया है जबकि प्राकृतिक इतिहास का निर्माण हमने नहीं किया है? तकनोलॉजी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार पर और उत्पादन की उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है, जिससे वह अपना जीवन-निर्वाह करता है, और इसतरह वह उसके सामाजिक सम्बन्धों तथा उनसे पैदा होने वाली मानसिक अवधारणाओं के निर्माण के प्रणाली को भी खोलकर रख देती है। यहाँ तक कि धर्म का इतिहास लिखने में भी यदि इस भौतिक आधार को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ऐसा प्रत्येक इतिहास आलोचनात्मक दृष्टि से वंचित हो जाता है। असल में जीवन के वास्तविक सम्बन्धों से इन सम्बन्धों के अनुरूप दैविक सम्बन्धों का विकास करने की अपेक्षा धर्म की धूमिल सृष्टि का विश्लेषण करके उसके लौकिक सार का पता लगाना कहीं अधिक आसान है। यही एकमात्र भौतिकवादी पद्धति है, और इसलिए यही एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति है। प्राकृतिक विज्ञान में अमूर्त भौतिकवाद ऐसा भौतिकवाद है जो इतिहास तथा उसकी प्रक्रिया को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। जब कभी उसके प्रवक्ता अपने विशेष विषय की सीमाओं के बाहर कदम रखते हैं, तब उनकी अमूर्त और वैचारिक अवधारणाओं से इस भौतिकवाद की त्रुटियाँ तुरंत स्पष्ट हो जाती हैं।
मार्क्स (पूँजी, खण्ड-एक, हिन्दी संस्करण, अध्याय 15 की पाद टिप्पणी सं.89, पृष्ठ 398-399, मास्को से प्रकाशित 1987 संस्करण)
↧
↧
इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धान्त
इतिहास का पहले का पूरा दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित था कि सभी तरह के ऐतिहासिक परिवर्तनों का मूल कारण मनुष्यों के परिवर्तनशील विचारों में ही मिलेगा और सभी तरह के ऐतिहासिक परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ही हैं तथा सम्पूर्ण इतिहास में उन्हीं की प्रधानता है। लेकिन लोगों ने यह प्रश्न न किया था कि मनुष्य के दिमाग में ये विचार आते कहाँ से हैं और राजनीतिक परिवर्तनों की प्रेरक शक्तियाँ क्या हैं। केवल फ्रांसीसी और कुछ-कुछ अंग्रेज इतिहासकारों की नवीनतर शाखा में यह विश्वास बरबस प्रविष्ट हुआ था कि कम से कम मध्ययुग से, सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए उदीयमान पूँजीपति वर्ग का सामंती अभिजात वर्ग के साथ संघर्ष यूरोप के इतिहास की प्रेरक शक्ति रहा है। मार्क्स ने सिद्ध कर दिया है कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है, अब तक के सभी विविधरूपी और जटिल राजनीतिक संघर्षों की जड़ में केवल सामाजिक वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक शासन की समस्या, पुराने वर्गों द्वारा अपना प्रभुत्व बनाये रखने तथा नये पनपते हुए वर्गों द्वारा इस प्रभुत्व को हस्तगत करने की समस्या ही रही है। लेकिन इन वर्गों के जन्म लेने और कायम रहने के कारण क्या हैं? इनका कारण वे शुद्ध भौतिक, गोचर परिस्थितियाँ हैं, जिनके अर्न्तगत समाज किसी भी युग मे अपने जीवन-यापन के साधनों का उत्पादन और विनिमय करता है। मध्ययुग के सामन्ती शासन का आधार छोटे-छोटे कृषक समुदायों की स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था था, जो अपनी ज़रूरत की प्राय: सभी चीज़ों का स्वयं उत्पादन कर लेते थे। इनमें विनिमय का प्राय: पूर्ण अभाव था, शस्त्रधारी सामन्त बाहर के आक्रमणों से इनकी रक्षा करते थे, उन्हें जातीय या कम से कम राजनीतिक एकता प्रदान करते थे। नगरों के अभ्युदय के साथ अलग-अलग दस्तकारियों और परस्पर व्यापार का विकास हुआ जो पहले आन्तरिक क्षेत्र में सीमित था और आगे चलकर अन्तरराष्ट्रीय हो गया। इस सब के साथ नगर के पूँजीपति वर्ग का विकास हुआ और मध्ययुग में ही उसने सामन्तों से लड़-भिड़कर सामन्ती व्यवस्था के अन्दर एक विशेषाधिकारप्राप्त श्रेणी के रूप में अपने लिए स्थान बना लिया। परन्तु 15वीं शताब्दी के मध्य के बाद से, यूरोप के बाहर की दुनिया का पता लगने पर, इस पूँजीपति वर्ग अपने अपने व्यापार के लिए कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र मिल गया। इससे उसे अपने उद्योग धन्धों के लिए नयी स्फूर्ति मिली। प्रमुख शाखाओं में दस्तकारी का स्थान मैनुफैक्चर ने ले लिया जो अब फैक्टरियों के पैमाने पर स्थापित था।फिर इसकी जगह बड़े पैमाने के उद्योग ने ले ली जो पिछली सदी के आविष्कारों, खासकर भाप से चलने वाले इंजन के आविष्कार से सम्भव हो गया था। बड़े पैमाने के उद्योग का व्यापार पर यह प्रभाव पड़ा कि पिछड़े हुए देशों में पुराना हाथ का काम ठप हो गया और उन्नत देशों में उसने संचार के आधुनिक नये साधन - भाप से चलने वाले जहाज, रेल, वैद्युतिक तार - उत्पन्न किये। इस प्रकार पूँजीपति वर्ग सामाजिक सम्पत्ति और सामाजिक शक्ति दोनों को अधिकाधिक अपने हाथों में केन्द्रित करने लगा, यधपि काफी अरसे तक राजनीतिक सत्ता से वह वंचित रहा जो सामंतों और उनके द्वारा समर्थित राजतंत्र के हाथ में थी। लेकिन विकास की एक मंजिल ऐसी आयी - फ्रांस में महान क्रान्ति के बाद - जब उसने राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लिया, और तब से वह सर्वहारा वर्ग और छोटे किसानों के ऊपर शासन करने वाला वर्ग बन गया। इस दृष्टिकोण से, समाज की विशेष आर्थिक स्थिति का सम्यक ज्ञान होने से सभी ऐतिहासिक घटनाओं से बड़ी सरलता से व्याख्या की जा सकती है, यधपि यह सही है कि हमारे पेशेवर इतिहासकारों में इस ज्ञान का सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार हर ऐतिहासिक युग की धारणाओं और उसके विचारों की व्याख्या बड़ी सरलता से, उस युग की आर्थिक जीवनावस्थाओं और सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर (ये सम्बन्ध भी आर्थिक परिस्थितियों द्वारा ही निर्धारित होते हैं), की जा सकती है। इतिहास को पहली बार अपना वास्तविक आधार मिला। यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य है जिसकी ओर पहले लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया था, यानी यह सत्य कि मनुष्यों को सबसे पहले खाना-पीना, ओढ़ना-पहनना और सिर के ऊपर साया चाहिए, इसलिए पहले उन्हें लाजि़मी तौर परकाम करना होता है, जिसके बाद ही वे प्रभुत्व के लिए एक दूसरे से झगड़ सकते हैं, और राजनीति, धर्म, दर्शन, आदि को अपना समय दे सकते हैं। आखि़रकार इस स्पष्ट सत्य को अपना ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त हुआ।
समाजवादी दृष्टिकोण के लिए इतिहास की यह नयी धारणा सर्वोच्च महत्व की थी। इससे पता लगा कि पहले के सम्पूर्ण इतिहास की गति वर्ग-विरोधों और वर्ग-संघर्षों के बीच में रही है, कि शासक और शासित, शोषक और शोषित वर्गों का अस्तित्व बराबर रहा है और यह कि मानव जाति के अधिकांश भाग के पल्ले सदा से कड़ी मशक़्क़त पड़ी है, आनन्दोपभोग बहुत कम। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि मानव जाति के विकास की सभी पिछली मंज़िलों में उत्पादन का विकास इतना कम हुआ था कि ऐतिहासिक विकास इस अन्तरविरोधी रूप में ही हो सकता था, ऐतिहासिक प्रगति कुल मिलाकर एक विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के क्रियाकलाप का ही विषय बना दी गयी थी, और बहुसंख्यकों के भाग्य में अपने श्रम द्वारा जीवन-निर्वाह के अपने स्वल्प साधन और इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार संपन्न समुदाय के लिए अधिकाधिक प्रचुर साधन उत्पादित करना रह गया था। परन्तु इतिहास की यही जांच-पड़ताल, जो हमें इस प्रकार पहले के वर्ग शासन की स्वाभाविक एवं बुद्धिसम्मत व्याख्या प्रदान करती है (अन्यथा हम मानव-स्वभाव की दुष्टता द्वारा ही उसकी व्याख्या कर सकते थे), साथ ही साथ हमें यह बोध कराती है कि वर्तमान युग में उत्पादन शक्तियों के अति प्रचण्ड विकास के कारण मानव-जाति को शासक और शासित, शोषक और शोषित में बांट रखने का अन्तिम बहाना भी, कम से कम सबसे उन्नत देशों में, मिट चुका है; कि शासक बड़े पूँजीपति अपनी ऐतिहासिक भूमिका समाप्त कर चुके हैं, और जैसा कि व्यापारिक संकटों, और खासकर पिछली भयानक गिरावट और सभी देशों में फैली मन्दी से सिद्ध हो चुका है, वे समाज का नेतृत्व करने के योग्य अब नहीं रह गये हैं, बल्कि उत्पादन के विकास में बाधक बन गये हैं; कि ऐतिहासिक नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के हाथ में चला गया है, ऐसे वर्ग के हाथ में चला गया है जो समाज में अपनी समग्र स्थिति के कारण सम्पूर्ण वर्ग शासन, सम्पूर्ण दासता एवं सम्पूर्ण शोषण का अन्त करके ही अपने को मुक्त कर सकता है; और यह कि सामाजिक उत्पादक शक्तियाँ, जो इतनी विकसित हो गयी हैं कि पूँजीपति वर्ग के काबू से बाहर है, बस इस प्रतीक्षा में है कि एकजुट सर्वहारा उन्हें अपने हाथों में ले ले जिससे कि ऐसी अवस्था कायम की जा सके जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य न केवल सामाजिक सम्पदा के उत्पादन में, बल्कि वितरण और प्रबन्ध में भी हाथ बंटा सकेगा, और जो अवस्था सम्पूर्ण उत्पादन के नियोजित संचालन द्वारा सामाजिक उत्पादक शक्तियों और उनकी उपज को इतना बढ़ा देगी कि प्रत्येक व्यक्ति की सभी उचित आवश्यक्ताओं की उत्तरोत्तर बढ़ती मात्रा में पूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी।
-फ्रेडरिक एंगेल्स ('कार्ल मार्क्स' 1877, ''volks-kalender'' नामक वार्षिकी के लिए लिखी गयी जीवनी)
समाजवादी दृष्टिकोण के लिए इतिहास की यह नयी धारणा सर्वोच्च महत्व की थी। इससे पता लगा कि पहले के सम्पूर्ण इतिहास की गति वर्ग-विरोधों और वर्ग-संघर्षों के बीच में रही है, कि शासक और शासित, शोषक और शोषित वर्गों का अस्तित्व बराबर रहा है और यह कि मानव जाति के अधिकांश भाग के पल्ले सदा से कड़ी मशक़्क़त पड़ी है, आनन्दोपभोग बहुत कम। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि मानव जाति के विकास की सभी पिछली मंज़िलों में उत्पादन का विकास इतना कम हुआ था कि ऐतिहासिक विकास इस अन्तरविरोधी रूप में ही हो सकता था, ऐतिहासिक प्रगति कुल मिलाकर एक विशेषाधिकारप्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के क्रियाकलाप का ही विषय बना दी गयी थी, और बहुसंख्यकों के भाग्य में अपने श्रम द्वारा जीवन-निर्वाह के अपने स्वल्प साधन और इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार संपन्न समुदाय के लिए अधिकाधिक प्रचुर साधन उत्पादित करना रह गया था। परन्तु इतिहास की यही जांच-पड़ताल, जो हमें इस प्रकार पहले के वर्ग शासन की स्वाभाविक एवं बुद्धिसम्मत व्याख्या प्रदान करती है (अन्यथा हम मानव-स्वभाव की दुष्टता द्वारा ही उसकी व्याख्या कर सकते थे), साथ ही साथ हमें यह बोध कराती है कि वर्तमान युग में उत्पादन शक्तियों के अति प्रचण्ड विकास के कारण मानव-जाति को शासक और शासित, शोषक और शोषित में बांट रखने का अन्तिम बहाना भी, कम से कम सबसे उन्नत देशों में, मिट चुका है; कि शासक बड़े पूँजीपति अपनी ऐतिहासिक भूमिका समाप्त कर चुके हैं, और जैसा कि व्यापारिक संकटों, और खासकर पिछली भयानक गिरावट और सभी देशों में फैली मन्दी से सिद्ध हो चुका है, वे समाज का नेतृत्व करने के योग्य अब नहीं रह गये हैं, बल्कि उत्पादन के विकास में बाधक बन गये हैं; कि ऐतिहासिक नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के हाथ में चला गया है, ऐसे वर्ग के हाथ में चला गया है जो समाज में अपनी समग्र स्थिति के कारण सम्पूर्ण वर्ग शासन, सम्पूर्ण दासता एवं सम्पूर्ण शोषण का अन्त करके ही अपने को मुक्त कर सकता है; और यह कि सामाजिक उत्पादक शक्तियाँ, जो इतनी विकसित हो गयी हैं कि पूँजीपति वर्ग के काबू से बाहर है, बस इस प्रतीक्षा में है कि एकजुट सर्वहारा उन्हें अपने हाथों में ले ले जिससे कि ऐसी अवस्था कायम की जा सके जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य न केवल सामाजिक सम्पदा के उत्पादन में, बल्कि वितरण और प्रबन्ध में भी हाथ बंटा सकेगा, और जो अवस्था सम्पूर्ण उत्पादन के नियोजित संचालन द्वारा सामाजिक उत्पादक शक्तियों और उनकी उपज को इतना बढ़ा देगी कि प्रत्येक व्यक्ति की सभी उचित आवश्यक्ताओं की उत्तरोत्तर बढ़ती मात्रा में पूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी।
-फ्रेडरिक एंगेल्स ('कार्ल मार्क्स' 1877, ''volks-kalender'' नामक वार्षिकी के लिए लिखी गयी जीवनी)
↧
'पहल' का अप्रैल अंक
↧
कुछ छोटी कविताएँ
चुप्पी
चुप्पी है घास
चुप्पी है कपास
और पानी की सलवटें
और काँपती उँगलियाँ
और कभी-कभी
एक अडिग फैसला भी।
उदासी
सहसा रात को
होता है घुटन का अहसास।
भरा होता है दिल
यादों से।
तपती होती है
पत्थर की एक पटिया
झील के तल में।
मिट्टी में दबा
लोहे का एक चाकू
जंग खाता रहता है।
और हम होते हैं
पतझड़ के पत्तों के बीच
ऊँघती वीरान सड़कों पर।
आश्चर्यलोक
हम चित्रों में जड़ दिये जायेंगे
किसी एक बृहस्पतिवार को
और इतवार आते-आते
छन्न से टूट कर गिर पड़ेंगे
फर्श पर।
यूँ हम आश्चर्य का सृजन करेंगे
और उसमें घुस जायेंगे
एलिस बनकर।
राहत
एक लहर आकर
सिर पटकेगी किनारे पर।
एक फुसफुसाहट गूँजेगी
सन्नाटे में।
आँसू का एक कतरा
पलकों पर चमकेगा
घास की नोंक पर ओस की बूँद की तरह।
जैसे युगों बाद
अँधेरे से बाहर आयेगी एक नाव
और हम एक लम्बी साँस लेंगे
राहत और चैन की,
एक लम्बे समय बाद।
हिंसा
वे घोड़े बहुत सुन्दर और प्यारे थे।
चिकनी रोएँदार चमड़ी,
चमकते-लहराते शानदार अयाल
और भीतर तक उतरती भावुक आँखों वाले।
उनके खुर
बना रहे थे लगातार
धरती के सीने पर घाव।
-कविता कृष्णपल्लवी
चुप्पी है घास
चुप्पी है कपास
और पानी की सलवटें
और काँपती उँगलियाँ
और कभी-कभी
एक अडिग फैसला भी।
उदासी
सहसा रात को
होता है घुटन का अहसास।
भरा होता है दिल
यादों से।
तपती होती है
पत्थर की एक पटिया
झील के तल में।
मिट्टी में दबा
लोहे का एक चाकू
जंग खाता रहता है।
और हम होते हैं
पतझड़ के पत्तों के बीच
ऊँघती वीरान सड़कों पर।
आश्चर्यलोक
हम चित्रों में जड़ दिये जायेंगे
किसी एक बृहस्पतिवार को
और इतवार आते-आते
छन्न से टूट कर गिर पड़ेंगे
फर्श पर।
यूँ हम आश्चर्य का सृजन करेंगे
और उसमें घुस जायेंगे
एलिस बनकर।
राहत
एक लहर आकर
सिर पटकेगी किनारे पर।
एक फुसफुसाहट गूँजेगी
सन्नाटे में।
आँसू का एक कतरा
पलकों पर चमकेगा
घास की नोंक पर ओस की बूँद की तरह।
जैसे युगों बाद
अँधेरे से बाहर आयेगी एक नाव
और हम एक लम्बी साँस लेंगे
राहत और चैन की,
एक लम्बे समय बाद।
हिंसा
वे घोड़े बहुत सुन्दर और प्यारे थे।
चिकनी रोएँदार चमड़ी,
चमकते-लहराते शानदार अयाल
और भीतर तक उतरती भावुक आँखों वाले।
उनके खुर
बना रहे थे लगातार
धरती के सीने पर घाव।
-कविता कृष्णपल्लवी
↧
↧
Article 0
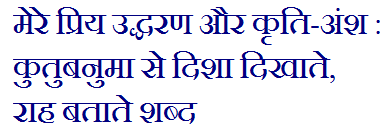 संघर्षरत और सृजनरत साथियों के लिएगोयठे की कुछ सूक्तियाँ
संघर्षरत और सृजनरत साथियों के लिएगोयठे की कुछ सूक्तियाँ- ज्ञान के साथ-साथ संदेह बढ़ता जाता है।
- जीवन जीवितों के लिए होता है और जो जीवित है उसे परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए।
- बुद्धिमान आदमी छोटी ग़लती नहीं करता।
- प्रतिभाशाली होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, यदि तुम किसी चीज़ की इज़्ज़त नहीं करते।
- वह सारा ज्ञान जो मेरे पास है, कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ़ मेरा है।
- ऐसे लोग कम होते हैं, जिनके पास यथार्थ के लिए कल्पना होती है।
- अपने आप पर विश्वास करना जादू है, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम कुछ भी सम्भव बना सकते हो।
- एक बेमतलब ज़न्िदगी अकाल मृत्यु के समान होती है।
- जीवन हमारी अनश्वरता की शैशवावस्था है।
↧
बड़े लोगों का भ्रष्टाचार बनाम आम आदमी का भ्रष्टाचार: कुछ फुटकल विचार
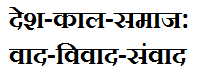 अन्ना हज़ारे और उन जैसे लोग भ्रष्टाचार की समस्या को पूरी पूँजीवादी व्यवस्था की बुनियादी कार्यप्रणाली से नहीं जोड़ते, अत: इसका समाधान वे जनलोकपाल जैसे एक विशालकाय नौकरशाही तंत्र के निर्माण में देखते है। दूसरा समाधान वे बताते हैं कि संसद में ईमानदार लोग चुनकर पहुंचें। तीसरा रास्ता वे ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार संपन्न बनाकर सत्ता के विकेंद्रीकरण का बताते हैं। एक बात और, अन्ना हज़ारे अक्सर यह कहते हैं कि सभी आम नागरिक यदि भ्रष्टाचार छोड़ देंगे तो पूरे देश से भ्रष्टाचार मिटाना आसान हो जाएगा।
अन्ना हज़ारे और उन जैसे लोग भ्रष्टाचार की समस्या को पूरी पूँजीवादी व्यवस्था की बुनियादी कार्यप्रणाली से नहीं जोड़ते, अत: इसका समाधान वे जनलोकपाल जैसे एक विशालकाय नौकरशाही तंत्र के निर्माण में देखते है। दूसरा समाधान वे बताते हैं कि संसद में ईमानदार लोग चुनकर पहुंचें। तीसरा रास्ता वे ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार संपन्न बनाकर सत्ता के विकेंद्रीकरण का बताते हैं। एक बात और, अन्ना हज़ारे अक्सर यह कहते हैं कि सभी आम नागरिक यदि भ्रष्टाचार छोड़ देंगे तो पूरे देश से भ्रष्टाचार मिटाना आसान हो जाएगा।पहली बात यह, यदि संसद सदस्य, मंत्री, अफसर और जज सभी भ्रष्ट हो सकते हैं तो जनलोकपाल के विशालकाय नौकरशाही तंत्र में भ्रष्टाचार के दीमक को घुसने से कदापि नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात यह कि, चुनाव में प्रत्याशी सदाचारी हैं, यह जानने का गारंटीशुदा तरीका क्या होगा? चुने जाने के बाद भी वह सदाचारी बना रहेगा, इसकी क्या गारंटी? सदाचारी-भ्रष्टाचारी होना जेनेटिक गुण नहीं है, इसके सामाजिक परिवेशगत कारण होते हैं। पूंजीवादी चुनाव प्रणाली में जिन भी देशों में जो भी सुधार किए गए हैं, कहीं भी आम आदमी ईमानदारी से चुनाव लड़कर अपवाद स्वरूप ही जीत सकता है। संसद या सरकार में यदि कोई ईमानदार आदमी पहुंच भी जाए तो वह पूरे सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक ढांचें में सर्वव्याप्त अनाचार-अत्याचार-भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकता। अन्ना हजारे अक्सर कहते रहते हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने छह भ्रष्ट मंत्रियों को हटने को बाध्य कर दिया। पूछा जा सकता है कि इससे फर्क क्या पड़ा? क्या महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार घट गया? एक भ्रष्ट की जगह दूसरा भ्रष्ट आ गया!
सामाजिक ढांचे में यदि असमानता, शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार, जातीय उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न आदि बने रहेंगे, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राम पंचायतों में सत्ता गांवों के दबंग कुलकों-भूस्वामियों के ही हाथों में केंद्रित रहेगी, आम गरीब अधिकांर-वंचित बने रहेंगे।
जब व्यक्त्यिों को सदाचारी बनने का उपदेश दिया जाता है, तो इस सच्चाई को झुठलाया जाता है कि सामाजिक-राजनीतिक ढांचा व्यक्तियों से ही बनता है, पर अलग-अलग व्यक्ति न तो अपने व्यक्तिगत आचरण से उस सामाजिक ढांचे को बदल सकते हैं, ना ही किसी विशेष सामाजिक ढांचे में वे मनचाहे तरीके से अपना व्यक्तिगत आचार-व्यवहार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आर्थिक-सामाजिक ढांचे और राजनीतिक-वैधिक प्रणाली द्वारा निर्धारित संस्कृति एवं आचार का अतिक्रमण अलग-अलग नागरिक व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते। कुछ लोग यदि करें भी तो इससे व्यापक स्तर पर कोई बदलाव नहीं आएगा। बुनियादी बात यह है कि राजसत्ता के वर्गचरित्र और समाज की वर्गीय संरचना की अनदेखी नहीं की जा सकती। पूंजीवादी समाज में देशी-विदेशी पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, राजसत्ता (सरकार, नौकरशाही, सेना-पुलिस, न्यायपालिका, विधायिका) उन्हीं के हितों की सेवा करती है, प्रचारतंत्र और संस्कृतितंत्र पर भी पूंजी का ही नियंत्रण है। 'कंट्रोलिंग टावर' राजसत्ता है। यह बल द्वारा स्थापित है, बल द्वारा चलती है, और बल द्वारा इसे ध्वंस करके तथा बल द्वारा ही अपनी राजसत्ता स्थापित करके बहुसंख्यक उत्पीड़ित जनसमुदाय कानूनी लूट (शोषण-उत्पीड़न-असमानता) और गैर-कानूनी लूट से छुटकारा पा सकता है। निरंतर जारीवर्ग संघर्ष और कुछ-कुछ ऐतिहासिक अंतरालों के बाद सामाजिक क्रांति के प्रचंड तूफानों के द्वारा ही इतिहास आगे डग भरता रहा है, और आगे भी ऐसा ही होगा।
समाज के धनी-मानी लोग -- नेता, अफसर, कारखानेदार, व्यापारी, ठेकेदार आदि जब भ्रष्टाचार से काला धन इकट्टा करते हैं तो वह काला धन देशी-विदेशी बैंकों के जरिए, शेयर बाजार के जरिए निवेशित होकर या रियल इस्टेट और सोने की खरीद में निवेशित होकर पूंजी के परिचलन के चक्र में शामिल हो जाता है। यह एक प्रकार का आदिम पूंजी संचय ही होता है।
लेकिन अक्सर यह एक आम आदमी के भ्रष्टाचार की -- एक चपरासी, एक सरकारी दफ्तर के बाबू, अस्पताल के कर्मचारी, आदि की भ्रष्टाचार की ही चर्चा होती है आम आदमी का आम आदमी के इसी भ्रष्टाचार से रोज-रोज का पाला पड़ता है। यह भ्रष्टाचार आम लोग आदिम पूंजी संचय के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए (जो कि महज तनख्वाह से पूरी नहीं हो पाती) या थोड़े बेहतर ढंग से जीने के लिए करते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि एक बार जब राह खुल जाती है और भटक भी खुल जाती है तो और बेहतर, और बेहतर तरीके से जी लेने के लिए, जहां तक संभव हो ''ऊपरी कमाई'' कर लेने की कोशिश एक चपरासी या एक क्लर्क भी करता है। हर समाज में सत्ताधारी वर्ग के विचार और संस्कृति ही जनसाधारण के आचार-व्यवहार को भी अनुकूलित-निर्धारित करते हैं। पूंजीवादी समाज में लोभ-लालच की संस्कृति का सर्वव्यापी वर्चस्व होता है। जिस समाज में किसी भी कीमत पर आगे बढ़े हुए को ही सम्मान मिलता हो, जहां शिक्षा-पद-ओहदा-सम्मान सब कुछ खरीदा-बेचा जाता हो, वहां एक-एक व्यक्ति को सदाचारी बनाने की नसीहत देकर पूरे समाज को दुरुस्त कर देना संभव नहीं है, वहां चंद लोगों के सदाचारी बन जाने से भी पूरे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वामपंथी ''मुक्त-चिंतक'' स्लावोक ज़जिेक की मूलभूत स्थापनाओं से मतभेद रखते हुए भी उसकी कुछ फुटकल उक्तियां मार्के की मालूम पड़ती हैं। आम समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जिजैक का कहना है : ''लोगों को और उनके रवैये को दोष मत दो''; ''भ्रष्टाचार या लालच समस्या नहीं है, समस्या वह व्यवस्था है जो भ्रष्ट होने के लिए धकेलती है। समाधान यह नहीं है कि ''मेन-स्ट्रीट या वालस्ट्रीट'', बल्कि उस व्यवस्था को बदलना समाधान है जिसमें मेन-स्ट्रीट या वालस्ट्रीट के बिना काम नहीं कर सकता।'' (वालस्ट्रीट न्यूयार्क की वह स्ट्रीट है जहां न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। 'मेनस्ट्रीट' आम सामाजिक जीवन के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वॉलस्ट्रीट के बिना मेनस्ट्रीट के चलने का तात्पर्य है वित्तीय पूंजी के वर्चस्व के बिना आम सामाजिक जीवन का चलना।)
समाज में उन्नत क्रांतिकारी चेतना पूरे पूंजीवादी ढांचे को तोड़ने के लिए व्यापक आम जनता की चेतना जब तक जागृत और संगठित नहीं करेगी, जब तक आम जनता की विघटित वर्ग-चेतना अपनी जिंदगी की तमाम बदहालियों-परेशानियों की मूल जड़ पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढांचे और राजनीतिक तंत्र में नहीं ढूंढ़ पाएगी, तब तक वह शासक वर्गों की संस्कृति और विचार को ही अपनाकर जीती रहेगी, तब तक आम लोगों से सदाचारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और इसका कोई मतलब भी नहीं होगा।
आम जनता के लिए सबसे बड़ा सदाचार और सबसे बड़ी नैतिकता यह है कि वह पूंजीवादी तंत्र को तबाह करके समाजवाद की स्थापना के लिए काम करे क्योंकि पूंजीवाद ही सभी अनाचारों-दुराचारों की जड़ है। जो लोग इस बात को समझ कर व्यापक जनएकजुटता और जनलामबंदी की कोशिशों में लग जाएंगे वे सपने में भी नहीं सोच सकते कि अपने ही जैसे किसी आम आदमी से मौके का लाभ उठाकर कुछ पैसे ऐंठ लिए जाएं। जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण उत्पीड़क चरित्र की असलियत नहीं बताते और उसकी तार्किक गति से चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार पर कुछ नियंत्रण लगाने की सुधारवादी कोशिशें करते हैं तथा साथ में जनता को भी सदाचार के उपदेश सुनाते रहते हैं, ये इस अनाचारी व्यवस्था के रक्षक के रूप में स्वयं बहुत बड़े अनाचारी होते हैं। वे सदाचार की टोपी पहनकर पूंजीवादी व्यवस्स्था के जर्जर खूनी चोगे की रफूगिरी व पैबंदसाजी करते रहते हैं और तरह-तरह के डिटर्जेंट इस्तेमाल करके उस पर लगे खून और गंदगी के धब्बे को साफ करते रहते हैं। वे डकैतों के चढ़ावे से बने मंदिरों में बैठकर उत्पीड़ित-वंचित जनता को सदाचार की ताबीज बांटते रहते हैं। वे ऐसे बावर्ची हैं जो सुधारवाद के पुराने व्यंजनों में नए-नए मसाले मिलाकर, उन्हें नई-नई विधियों से पकाकर, नए-नए जायके पैदा करते रहते हैं।
↧
दिल धड़कने का सबब
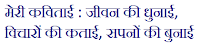 किसके लिए धड़कता है मेरा दिल?
किसके लिए धड़कता है मेरा दिल?सन्नाटे पर सलवटें डालती थरथराती लहरों के लिए,
एक पुराने फाउण्टेन पेन के लिए,
ज़िन्दगी की उदासियों के बीच
कुछ मनभावन बग़ावती ख़यालों के लिए,
कुछ छविध्वंसक और कुछ मूर्तिभंजक इच्छाओं के लिए,
वीराने में भेड़ चराते गड़रिये जैसे
गुज़रे दिनों और भूतपूर्व दोस्तों की यादों के लिए,
छोटे-छोटे पुलों जैसे आने वाले दिनों के लिए,
सिर्फ कल्पना में जीवित पहाड़ी कस्बों के लिए,
ऊन के सफेद गोलों से लुढ़कते पिल्लों जैसे
भागते-उलझते विचारों के लिए,
हर रात कुछ खुशनुमा सपनों की उम्मीद मे
नींद के इंतजार के लिए।
- कविता कृष्णपल्लवी
↧
उत्पादन: इसका तर्क और इसका इतिहास
शब्द के सर्वाधिक अभिधात्मक अर्थ में मनुष्य एक zoonpolitikonहोता है, और न केवल एक सामाजिक प्राणी होता है बल्कि ऐसा प्राणी होता है जो सिर्फ समाज के भीतर ही एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकता है। समाज के बाहर अलग-थलग व्यक्तियों द्वारा उत्पादन का विचार उतना ही भीषण बेतुका विचार है जितना व्यक्तियों के एक साथ रहे बिना और परस्पर बातचीत किये बिना भाषा के विकास का विचार - ऐसा अपवादस्वरूप केवल तभी हो सकता है, जब एक सभ्य व्यक्ति जिसने पहले ही समाज की शक्तियों को गतिशील ढंग से अपने में सन्निहित कर लिया हो, संयोगवश किसी बीहड़ एकाकी स्थान में पहुँच जाये। इस मुद्दे पर आगे और विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत ही नहीं होती, अगर उस सनक को, जिसका औचित्य और अर्थ सिर्फ 18वीं शताब्दी के लोगों के लिए था, पूरी तत्परता के साथ बास्तियात, कैरे, प्रूधों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिरोपित नहीं किया गया होता। प्रूधों और दूसरे लोग जब किसी खास आर्थिक परिघटना के ऐतिहासिक मूल को नहीं जानते, तो मिथकशास्त्र में जाकर उसकी अधकचरी ऐतिहासिक-दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करने में स्वाभाविक तौर पर काफी आनन्द महसूस करते हैं। आदम या प्रोमेथियस को एक बनी-बनायी स्कीम मिल गयी जिसे उन्होने अपना लिया, वगैरह। लोकोत्तीय बुद्धिमत्ता के स्वप्न देखने से अधिक नीरस-उबाउ और कुछ नहीं होता।
इसलिए, जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सामाजिक विकास की एक ख़ास मंजिल में उत्पादन, या सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन होता है। इसलिए यह लग सकता है कि उत्पादन की बात करने के लिए, हमें या तो विकास की ऐतिहासिक प्रकिृया के विभिन्न चरणों का पता लगाना चाहिए, या शुरू में ही घोषणा कर देनी चाहिए कि हम एक ख़ास ऐतिहासिक काल, जैसे उदाहरण के लिए आधुनिक पूँजीवादी उत्पादन, का अध्ययन कर रहे हैं, जो वास्तव में इस कृति की विषय-वस्तु है। तो भी उत्पादन की सभी मंजिलों की कुछ सुनिश्चित समान विशेषताएँ होती हैं, कुछ समान उद्देश्य होते हैं। आम तौर पर उत्पादन एक अमूर्तन होता है, लेकिन वह एक तार्किक अमूर्तन होता है, क्योंकि वह समान अभिलाक्षणिकताओं को छाँटकर अलग करता है और सुनिश्चत करता है, तथा इस तरह हमें दुहराव से बचाता है। तथापि तुलना द्वारा उद्घाटित की गयी ये सामान्य या आम अभिलाक्षणिकताएँ एक बहुत जटिल चीज़ को संघटित करती हैं जिसके संघटक तत्वों के अलग-अलग गंतव्य या भवितव्य होते हैं। इनमें से कुछ तत्व सभी युगों में पाये जाते हैं, कुछ अन्य तत्व कुछ युगों में पाये जाते हैं। इनमें से कुछ तत्व सर्वाधिक आधुनिक युग में भी मौजूद हैं और सर्वाधिक प्राचीन युगों में भी मौजूद थे। उनके बिना उत्पादन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ सर्वाधिक सम्पूर्ण विकसित भाषाओं और सबसे कम विकसित भाषाओं के बीच भी कुछ नियम और शर्ते समान होती हैं, वहीं सामान्य और आम से उनके प्रस्थान बिन्दु उनके विकास की अभिलाक्षणिकता होते हैं। आम तौर पर उत्पादन को विनियमित करने वाली स्थितियों का विभेदीकरण किया जाना चाहिए ताकि उस सामान्य एकरूपता के चलते अन्तर के बुनियादी बिन्दु दृष्टिओझल न हो जायें, जो सामान्य एकरूपता इस तथ्य के नाते होती है कि हर स्थिति में कर्त्ता , मानवजाति और लक्षित वस्तु, प्रकृति - ये दोनों चीज़ें समान होती हैं।
इस तथ्य को याद रख पाने में विफलता आधुनिक अर्थशास्त्रियों की उस सारी अक्लमंदी का स्रोत है जो मौजूद सामाजिक स्थितियों की शाश्वत प्रकृति और सामंजस्य को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह, मिसाल के तौर पर, वे कहते हैं कि उत्पादन के किसी उपकरण के बिना कोई भी उत्पादन सम्भव नहीं होता, भले ही वह उपकरण केवल हाथ हो; कि अतीत के संचित श्रम के बिना कुछ भी सम्भव नहीं होता, भले ही यह श्रम मात्र वह कौशल हो, जो बार-बार प्रयोग द्वारा किसी जंगली मनुष्य के हाथों में संचित और संकेन्द्रित हुआ हो। पूँजी, अन्य चीज़ों के अलावा, उत्पादन का उपकरण भी होती है, अतीत का निर्वैत्तिक श्रम भी होती है। अत: पूँजी एक सार्वभौमिक, शाश्वत, प्राकृतिक परिघटना है; यह सच होगा यदि हम उन विशिष्ट गुणों की अनदेखी कर दें जो एक ''उत्पादन के उपकरण''को और ''संचित श्रम''को पूँजी में बदल देते हैं।
-मार्क्स ('राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान', 1859)
इसलिए, जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सामाजिक विकास की एक ख़ास मंजिल में उत्पादन, या सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन होता है। इसलिए यह लग सकता है कि उत्पादन की बात करने के लिए, हमें या तो विकास की ऐतिहासिक प्रकिृया के विभिन्न चरणों का पता लगाना चाहिए, या शुरू में ही घोषणा कर देनी चाहिए कि हम एक ख़ास ऐतिहासिक काल, जैसे उदाहरण के लिए आधुनिक पूँजीवादी उत्पादन, का अध्ययन कर रहे हैं, जो वास्तव में इस कृति की विषय-वस्तु है। तो भी उत्पादन की सभी मंजिलों की कुछ सुनिश्चित समान विशेषताएँ होती हैं, कुछ समान उद्देश्य होते हैं। आम तौर पर उत्पादन एक अमूर्तन होता है, लेकिन वह एक तार्किक अमूर्तन होता है, क्योंकि वह समान अभिलाक्षणिकताओं को छाँटकर अलग करता है और सुनिश्चत करता है, तथा इस तरह हमें दुहराव से बचाता है। तथापि तुलना द्वारा उद्घाटित की गयी ये सामान्य या आम अभिलाक्षणिकताएँ एक बहुत जटिल चीज़ को संघटित करती हैं जिसके संघटक तत्वों के अलग-अलग गंतव्य या भवितव्य होते हैं। इनमें से कुछ तत्व सभी युगों में पाये जाते हैं, कुछ अन्य तत्व कुछ युगों में पाये जाते हैं। इनमें से कुछ तत्व सर्वाधिक आधुनिक युग में भी मौजूद हैं और सर्वाधिक प्राचीन युगों में भी मौजूद थे। उनके बिना उत्पादन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ सर्वाधिक सम्पूर्ण विकसित भाषाओं और सबसे कम विकसित भाषाओं के बीच भी कुछ नियम और शर्ते समान होती हैं, वहीं सामान्य और आम से उनके प्रस्थान बिन्दु उनके विकास की अभिलाक्षणिकता होते हैं। आम तौर पर उत्पादन को विनियमित करने वाली स्थितियों का विभेदीकरण किया जाना चाहिए ताकि उस सामान्य एकरूपता के चलते अन्तर के बुनियादी बिन्दु दृष्टिओझल न हो जायें, जो सामान्य एकरूपता इस तथ्य के नाते होती है कि हर स्थिति में कर्त्ता , मानवजाति और लक्षित वस्तु, प्रकृति - ये दोनों चीज़ें समान होती हैं।
इस तथ्य को याद रख पाने में विफलता आधुनिक अर्थशास्त्रियों की उस सारी अक्लमंदी का स्रोत है जो मौजूद सामाजिक स्थितियों की शाश्वत प्रकृति और सामंजस्य को सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह, मिसाल के तौर पर, वे कहते हैं कि उत्पादन के किसी उपकरण के बिना कोई भी उत्पादन सम्भव नहीं होता, भले ही वह उपकरण केवल हाथ हो; कि अतीत के संचित श्रम के बिना कुछ भी सम्भव नहीं होता, भले ही यह श्रम मात्र वह कौशल हो, जो बार-बार प्रयोग द्वारा किसी जंगली मनुष्य के हाथों में संचित और संकेन्द्रित हुआ हो। पूँजी, अन्य चीज़ों के अलावा, उत्पादन का उपकरण भी होती है, अतीत का निर्वैत्तिक श्रम भी होती है। अत: पूँजी एक सार्वभौमिक, शाश्वत, प्राकृतिक परिघटना है; यह सच होगा यदि हम उन विशिष्ट गुणों की अनदेखी कर दें जो एक ''उत्पादन के उपकरण''को और ''संचित श्रम''को पूँजी में बदल देते हैं।
-मार्क्स ('राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान', 1859)
↧
↧
'पहल'का जून अंक
↧
'पहल' का जुलाई अंक
↧
आधुनिक ऐतिहासिक विकासों ने इतिहास के विज्ञान को सम्भव बनाया
जब हम प्रकृति या मानव-जाति के इतिहास पर या अपने मन की प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं तब पहले हमें क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, सम्बन्धों, विभिन्न तत्वों के योग और संयोजन से बना हुआ एक जाल-सा दिखाई देता है, जो कहीं ख़त्म नहीं होता, जिसमें कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती, जो जहाँ जैसा था, वह वहाँ वैसा नहीं रहता, हर वस्तु गतिशील है, परिवर्तनशील है, हर वस्तु का निर्माण होता है और नाश होता है। इस प्रकार हम इस चित्र को पहले समग्र रूप में देखते हैं, उसके अलग-अलग हिस्से हमारी नज़र में नहीं पड़ते, वह न्यूनाधिक पृष्ठभूमि में ही रहते हैं। हम गति, संक्रमण और परस्पर सम्बन्धों को देखते हैं, किन्तु जिन वस्तुओं की यह गति है, यह योग और सम्बन्ध हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते। विश्व की यह धारणा आदिम और भोली-भाली है, लेकिन मूलतः वह ग़लत नहीं हैं, और प्राचीन यूनानी दर्शन की धारणा भी यही थीं, जिसे स्पष्ट रूप से सबसे पहले हेराक्लाइटस ने प्रतिपादित किया था। उसने कहा था - हर वस्तु है और नहीं भी है, क्योंकि हर वस्तु अस्थिर है, सतत परिवर्तनशील है, सतत निर्माण और नाश की अवस्था में है।
लेकिन यह धारणा कुल मिलाकर दृश्य-जगत के चित्र के सामान्य स्वरूप को तो सही-सही व्यक्त करती है, लेकिन जिन तफ़सीलों से यह चित्र बना है, उनका विवरण देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और जब तक हम इन्हें नहीं समझें, हम पूरे चित्र को साफ़ तौर पर समझ नहीं सकते। इन तफ़सीलों को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उन्हें उनके प्राकृतिक या ऐतिहासिक सम्बन्धों से अलग करें और हर तफ़सील पर, चित्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग पर अलग-अलग विचार करें;उसके स्वरूप, उसके विशेष कारणों, कार्यों इत्यादि की, पृथक् रूप से परीक्षा करें। यह काम ख़ास तौर पर प्रकृति-विज्ञान और ऐतिहासिक अनुसन्धान का है, और यही विज्ञान की वह शाखाएँ हैं, जिन्हें प्राचीन काल के यूनानियों ने एक निचले दरजे में डाल दिया था, और इसका यथेष्ट कारण भी था, क्योंकि उन्हें सबसे पहले इन विज्ञानों के लिए सामग्री एकत्र करनी थी, जिसके आधार पर वह कार्य कर सकें। प्रकृत्ति और इतिहास के सम्बन्ध में जब तक पहले कुछ सामग्री एकत्र न हो ले, तब तक आलोचनात्मक विश्लेषण, तुलना और वर्गों, श्रेणियों और जातियों के रूप में वर्गीकरण नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविकता का यथातथ्य वर्णन करनेवाले प्रकृति-विज्ञान का आधार सबसे पहले अलेक्ज़ेण्ड्रियन काल* के यूनानियों ने और बाद में मध्ययुग के अरबों ने स्थापित किया। अपने यथार्थ रूप में प्रकृति-विज्ञान का आरम्भ पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्धसे ही होता है, और तब से इस विज्ञान ने लगातार बढ़ती हुई रफ़्तार से तरक्कीकी है। प्रकृति का विश्लेषण करके उसके अलग-अलग भाग करना, विभिन्न वस्तुओं और प्रक्रियाओं को निश्चित वर्गों या समूहों में एकत्रकरना, अपने विविधरूपों में कार्बनीय पिण्डों की आन्तरिक शरीर-रचना का अध्ययन करना - पिछले चार सौ वर्षों में प्रकृति सम्बन्धीहमारे ज्ञान में जो विराट प्रगति हुई है, उसकी यह बुनियादी शर्ते थीं। परन्तु इस कार्य-प्रणाली ने हमारे लिए एक विरासत भी छोड़ी है - उसने हमारे अन्दर ऐसी आदत डाल दी है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं और प्रक्रियाओं को, सम्पूर्ण वास्तविकता से उनके सम्बन्ध को विच्छिन्न करके देखते हैं, उन्हें गति की नहीं विराम की स्थिति में, मूलत: परिवर्तनशील नहीं बल्कि स्थिर अवस्था में, जीवन की नहीं मृत्यु की अवस्था में देखते हैं। और जब बेकन और लाक इस दृष्टिकोण को प्रकृति-विज्ञान के क्षेत्रसे दर्शन के क्षेत्रमें ले आये, तब उस संकीर्ण, अधिभूतवादी विचार-प्रणाली का जन्म हुआ, जो पिछली शताब्दी की एक विशेषता रही है।
अधिभूतवादी के लिए वस्तु और वस्तुओं के मानस-चित्र, अर्थात् विचार, एक दूसरे से विच्छिन्न और स्वाधीन हैं। वह उन्हें अनुसन्धान की स्थिर, निश्चित और अपरिवर्तनीय सामग्री मानता है; उन्हें एक दूसरे से अलग करके और एक के बाद एक देखता है। उसका चिन्तन ऐसे प्रतिवादों के रूप में होता है, जिनका परस्पर सामंजस्य हो ही नहीं सकता। ''वह बात करता है, तो 'हाँ' में, या 'नहीं' में, और जो न 'हाँ' में है, और न 'नहीं' में, वह शैतान की शरारत है।''उसकी दृष्टि में या तो किसी वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है, कोई वस्तु एक ही समय में जो वह है, उससे भिन्न नहीं हो सकती, भाव और अभाव पक्ष दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं, दोनोंमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। कार्य और कारण की कोटियाँ एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों में कड़ा विरोध है।
पहली नज़र में यह विचार-प्रणाली अत्यन्त परिष्कृत और स्पष्ट मालूम होती है, क्योंकि यह प्रणाली तथाकथित स्वस्थ व्यवहार-बुद्धि की प्रणाली है। परन्तु यह स्वस्थ व्यवहार-बुद्धि अपने घर की चहारदीवारी के अन्दर तो एक विश्वसनीय सहायक के रूप में बड़े मज़े से रह लेती है, लेकिन जहाँ उसने अनुसन्धान के विशाल जगत में पदार्पण किया नहीं कि वह बड़े ख़तरे में पड़ जाती है। कुछ क्षेत्रोंमें, जिनका विस्तार इस बात पर निर्भर है कि अनुसन्धान के विशिष्ट विषय का स्वरूप क्या है, अधिभूतवादी विचार-प्रणाली आवश्यक और उचित भी है, परन्तु न्यूनाधिक काल के बाद यह प्रणाली एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाती है जिसके आगे ले जाने पर वह एकांगी, संकुचित, अमूर्त और अवास्तविक हो जाती है, और अमिट विरोधोंके भँवर मेंपड़कर अपना रास्ता खो बैठती है। अलग-अलग वस्तुओं पर विचार करते समय अधिभूतवादी उनके परस्पर सम्बन्धोंको भूल जाता है, उनके अस्तित्व पर विचार करते समय वह उस अस्तित्व के आरम्भ और अन्त को भूल जाता है, उन्हें विराम-स्थिति में देखता है, लेकिन उनकी गति को भूल जाता है। वह वृक्षों के पीछे वन को नहीं देख पाता।
मिसाल के तौर पर अपने रोजमर्रा के काम के लिए हम यह जानते हैं और कह सकते हैं कि कोई प्राणी जीवित है या नहीं। लेकिन गौर से देखने पर यह मालूम होता है कि यह अक्सर एक बहुत पेचीदा सवाल होता है। कानूनदाँ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने इस बात को लेकर बहुत माथापच्ची की है कि वह मुनासिब हद कौन-सी है, जिसके आगे माँ के गर्भ के बच्चे को नष्ट करने का मतलब है हत्या करना; और फिर भी वह इसको निश्चित नहीं कर पाये हैं। इसी प्रकार मृत्यु के क्षण को सम्पूर्ण रूप से निश्चित करना असम्भव है, क्योंकि शरीर-विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मृत्यु कोई आकस्मिक और क्षणभर में हो जाने वाली घटना नहीं है, वह एक बहुत लम्बी प्रक्रिया है।
इसी प्रकार प्रत्येक कार्बनीय पदार्थ हर क्षण में, जो वह है, उससे भिन्न भी है। वह हर क्षण बाहर से कुछ पदार्थ ग्रहण करता है और भीतर से कुछ अन्य पदार्थ खारिज करता है। हर क्षण उसके शरीर के कुछ जीव-कोष मरते रहते हैं और कुछ नये जीव-कोष पुनर्निर्मित होते रहते हैं और इस तरह न्यूनाधिक समय में उसके शरीर का पदार्थ फिर से बिल्कुल नया हो जाता है, पुराने पदार्थ की जगह नये पदार्थ के अणु ले लेते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्बनीय पदार्थ किसी समय में जो वह है, उससे भिन्न भी है।
इतना ही नहीं, सूक्ष्मतर निरीक्षण के बाद यह भी पता चलता है कि किसी प्रतिवाद के दोनों छोर, भाव-पक्ष और अभाव-पक्ष, जैसे एक-दूसरे के विरोधीहैं, वैसे ही अभिन्न भी, और अपने सारे विरोध के बावजूद वे एक-दूसरे में अन्तरव्याप्त हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कार्य तथा कारण की धारणाएँ तभी सार्थक हैं, जब हम उन्हें विशेष घटनाओं पर लागू करें। लेकिन जहाँ हम इन विशेष घटनाओं को समग्र रूप में अर्थात विश्व के साथ सम्बद्धरूप में देखते हैं, वे एक-दूसरे से टकरा जाते हैं, और उनमें खासकर तब और भी गड़बड़ हो जाती है, जब हम उस विश्व-व्यापी क्रिया और प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं जिनमें कारण और कार्य निरन्तर स्थान बदलते रहते हैं। जो एक समय और एक स्थान पर कार्य है, वही दूसरे समय और दूसरे स्थान पर कारण बन जाता है। और इसी तरह जो कारण है, वह कार्य बन जाता है।
अधिभूतवादी तर्क-पद्धति का ढाँचा तैयार करने में इन विचार-प्रक्रियाओंऔर प्रणालियों का कोई हाथ नहीं है। इसके विपरीत द्वन्द्ववाद वस्तुओं और उनके मानस-चित्रों, अर्थात विचारों को, उनके बुनियादी सम्बन्ध, गति, आरम्भ और अन्त को ध्यान में रखकर ही ग्रहण करता है। इसलिए ऊपर जिन प्रक्रियाओं का हमने उल्लेख किया है, वे द्वन्द्ववाद की अपनी कार्यप्रणाली का समर्थन करती हैं।
द्वन्द्ववाद का प्रमाण प्रकृति है, और यह मानना ही होगा कि आधुनिक विज्ञान ने इस प्रमाण के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत की है और यह सामग्री प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार विज्ञान ने यह दिखा दिया है कि अन्तत: प्रकृति अधिभूतवादी रूप से नहीं, द्वन्द्वात्मक रूप से कार्य करती है; वह एक सदा पुनरावर्तित वृत्त के अपरिवर्तनशील क्रम में चक्कर नहीं काटती, बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक विकास के क्रम से गुजरती है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले डार्विन का नाम लेना होगा। उन्होंने यह सिद्धकर दिया कि सभी कार्बनीय सत्ताएँ-वनस्पति, जीव तथा स्वयं मनुष्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई हैं, जो करोड़ों साल से चलती आ रही है। इस तरह उन्होंने प्रकृति की अधिभूतवादी धारणा पर सबसे कठोर आघात किया। परन्तु ऐसे प्रकृतिज्ञानी बहुत कम हैं, जिन्होंने द्वन्द्वात्मक रूप से विचार करना सीख लिया है, और अनुसन्धान के निष्कर्षों तथा पूर्वकल्पित विचार-पद्धतियों के बीच इस विरोध के कारण प्रकृति-विज्ञान के सैद्धान्तिक क्षेत्रमें बेहद गड़बड़ी फैली हुई है, जिससे शिक्षक तथा शिक्षार्थी, लेखक तथा पाठक, सभी को निराशा होती है।
इसलिए विश्व का, उसके विकास का, मानव-जाति के विकास का, और मानव-मन पर इस विकास के प्रतिबिम्ब का, सच्चा चित्रद्वन्द्वात्मक प्रणाली के द्वारा ही मिल सकता है क्योंकि यही प्रणाली जीवन और मृत्यु, पुरोगामी और प्रतिगामी परिवर्तनों की असंख्य क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं को सदा ध्यान में रखती है। नवीन ज़र्मन दर्शन इसी भावना को लेकर चला है। अपना दार्शनिक जीवन आरम्भ करते ही काण्ट ने न्यूटन की एक स्थायी सौर-मण्डल की धारणा को बदल डाला।न्यूटन का विचार था कि यह सौर-मण्डल, एक बार आरम्भ में उसे जो वेग मिला-प्राथमिक वेग का यह सिद्धान्त प्रसिद्धहो चुका है - उसके बाद से एक शाश्वत सतत अपरिवर्तनशील क्रम से चल रहा है। लेकिन काण्ट ने कहा कि यह सौर-मण्डल एक ऐतिहासिक क्रम का, एक चक्कर काटते हुए वाष्पपुंज से सूर्य तथा सभी ग्रहों के निर्माण का परिणाम है। इससे उन्होंने साथ ही यह निष्कर्ष भी निकाला कि यदि सौर-मण्डल की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है, तो भविष्य में उसका विनाश भी निश्चित है। आधीशताब्दी बाद, लैपलेस ने काण्ट के इस सिद्धान्त को गणित के आधार पर प्रमाणित कर दिया और इसके भी आधीशताब्दी बाद वर्णक्रमलेखी(स्पेक्ट्रोस्कोप) का आविष्कार होने पर यह प्रमाणित हो गया कि बाह्य अन्तरिक्ष में ऐसे चमकते हुए वाष्पपुंज हैं, और यह वाष्पपुंज घनीकरण की विभिन्न अवस्थाओं में है।
इस नये जर्मन दर्शन का चरम विकास हेगेल की चिन्तन-प्रणाली में हुआ। इस प्रणाली में - और यही इसकी बहुत बड़ी ख़ूबी है - यह पूरा जगत-प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा मानसिक जगत - पहली बार एक प्रक्रिया के रूप में, अर्थात सतत प्रवाह, गति, परिवर्तन तथा विकास की अवस्था में चित्रित किया गया है, और साथ ही उस आन्तरिक सम्बन्ध को, उस सूत्रको पकड़ने की कोशिश की गयी है, जिससे इस समस्त गति और विकास को एक क्रमबद्धव्यवस्था का रूप मिल सके। इस दृष्टिकोण से मानव-जाति का इतिहास निरर्थक, हिंसक कार्यों का आवर्त न रह गया - ऐसे कार्यों का आवर्त जो परिपक्वदार्शनिक बुद्धि के न्याय-सिंहासन के सम्मुख सब के सब समान रूप से हेय तथा निन्दनीय हैं, और जिन्हें शीघ्रसे शीघ्र भूल जाना ही श्रेयस्कर है - बल्कि इस दृष्टि से यह इतिहास स्वयं मनुष्य के विकास की प्रक्रिया के रूप में दीख पड़ा। अब यह काम बुद्धि का था कि वह इस प्रक्रिया के टेढ़े-मेढ़े रास्ते से क्रमिक विकास की गति को परखे, और जो घटनाएँ ऊपर से देखने में आकस्मिक जान पड़ती हैं उनमें अन्तरनिहित नियमितता को खोज निकाले।
हेगेल की प्रणाली ने जिस समस्या को विचार के लिए प्रस्तुत किया, उसे वह सुलझा न पायी, लेकिन इस बात का कोई महत्व नहीं हैं। उसका युगान्तरकारी महत्व इस बात में है कि उसने उस समस्या को प्रस्तुत किया। यह समस्या ही ऐसी है कि कोई एक व्यक्ति उसे कभी सुलझा नहीं पायेगा। सेण्ट-साइमन के साथ, हेगेल अपने युग में सबसे व्यापक चेतना रखनेवाले व्यक्ति थे, जिनका मस्तिष्क सचमुच विराट था; तब भी वह सबसे पहले अपने ज्ञान की अनिवार्य सीमा से, और दूसरे अपने युग के, विस्तार और गहराई, दोनों में सीमित ज्ञान और धारणाओं की सीमा से बँधेहुए थे। इनके बाद एक तीसरी सीमा भी थी। हेगेल आदर्शवादी थे। उनके निकट मानव-मस्तिष्क के विचार वास्तविक वस्तुओं और क्रियाओं के न्यूनाधिक निराकार प्रतिबिम्ब न थे, उल्टे यह वस्तुएँ और उनका विकास किसी''विचार'' का व्यक्त, मूर्त और प्रतिफलित रूप था, और इस ''विचार''का संसार के पहले से ही, अनादि काल से अस्तित्व रहा है। इस चिन्तन-प्रणाली ने हर चीज़ को सिर के बल खड़ा कर दिया, और संसार में वस्तुओं के यथार्थ सम्बन्ध को बिल्कुल उलट डाला। और यद्यपि हेगेल ने कितने ही विशिष्ट तथ्य-समूहों को ठीक-ठीक और बड़ी सूझ-बूझ के साथ समझा,फिर भी उपरोक्त कारणों से हेगेल की रचनाओं में बहुत कुछ ऐसा है, जो भोंड़ा है, बनावटी है, जबर्दस्ती किसी तरह ठूँसा गया है - एक शब्द मेंकहें तो तफसीली बातों में ग़लत है। हेगेल की प्रणाली में विचारों का एक भयंकर गर्भपात हुआ हैं, परन्तु यह अन्तिम बार ऐसा हुआ। वास्तव में यह प्रणाली एक ऐसे आन्तरिक विरोध से पीड़ित थी, जिसका कोई इलाज़ न था। एक ओर उसकी मूल स्थापना यह धारणा थी कि मानव-इतिहास विकास की एक प्रक्रिया है, जिसकी स्वभावत: यह परिणति कभी नहीं हो सकती कि किसी तथाकथित निरपेक्ष सत्य के आविष्कार को बुद्धि की चरम सीमा मान ली जाये। परन्तु दूसरी ओर इस प्रणाली का यह दावा था कि वह इसी निरपेक्ष सत्य का सार है। प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली, जो सर्वव्यापी हो, सदा के लिए निश्चित हो और अन्तिम सत्य हो, द्वन्द्ववादी तर्क-पद्धति के मूलभूत नियम के प्रतिकूल है। और यह विचार कि बाह्य जग़त के विषय में हमारा व्यवस्थित ज्ञान, एक युग से दूसरे युग तक विराट प्रगति कर सकता है, इस नियम से बाहर नहीं, प्रत्युत उसके अन्तर्गत है।
जर्मन आदर्शवाद के इस मौलिक अन्तरविरोध की उपलब्धि का फल यह हुआ कि दार्शनिकों का झुकाव फिर भौतिकवाद की ओर हुआ, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह भौतिकवाद अठारहवीं सदी के अधिभूतवादी, बिल्कुल यांत्रिक भौतिकवाद से भिन्न था। पुराने भौतिकवाद की दृष्टि मेंसमस्त पूर्वकालीन इतिहास हिंसा और निर्बुद्धिताका एक पुंज है, परन्तु आधुनिक भौतिकवाद की दृष्टि में यह इतिहास मानव-जाति के विकास की एक निश्चित प्रक्रिया है, और उसका लक्ष्य है इस विकास के नियमों का पता लगाना। अठारहवीं शताब्दी के फ्रांसीसियों की और हेगेल तक की यह धारणा थी कि सम्पूर्ण प्रकृति एक सीमित वृत्त में घूमती है और सदा के लिए अपरिवर्तनशील है; जैसा न्यूटन ने कहा था, उसके आकाशीय पिण्ड नित्य हैं; और जैसा लिन्नीयस ने कहा था, सभी कार्बनीय जातियाँ नित्य और अपरिवर्तनशील हैं। आधुनिक भौतिकवाद ने प्रकृति-विज्ञान के हाल के अनुसन्धानों को ग्रहण किया है, जिनके अनुसार काल के प्रवाह में प्रकृति का भी एक इतिहास है, वह भी काल के अधीन है, और आकाशीय पिण्ड, उन कार्बनीय जातियों की तरह ही, जो अनुकूल परिस्थितियों में उनमें वास करते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। और अगर अभी भी यह कहना होगा कि सम्पूर्ण प्रकृति निरन्तर पुनरावर्तित होनेवाले वृत्तोंमें घूमती है, तो साथ ही यह भी मानना होगा कि यह वृत्त निरन्तर वृहत्तर होते जाते हैं। दोनों पहलू से आधुनिक भौतिकवाद मूलत: द्वन्द्वात्मक है, और अब उसे ऐसे दर्शन की आवश्यकता न रह गयी, जो शेष सभी विज्ञानों पर शासन करने का दम भरे। जैसे ही प्रत्येक विज्ञान, वस्तुओं की विस्तृत समष्टि में, और उनके ज्ञान की समष्टि में, अपना स्थान स्पष्ट कर लेता है, वैसे ही इस समष्टि से सम्बन्ध रखनेवाले एक विशेष विज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती और वह बेकार हो जाता है। पुराने दर्शन का अगर कोई भाग बचा रहता है, तो वह है विचार तथा उसके नियमों का विज्ञान-तर्क-शास्त्रऔर द्वन्द्ववाद। बाकीसब कुछ प्रकृति तथा इतिहास के प्रत्यक्ष विज्ञान का अंग बन जाता है।
यद्यपि प्रकृति सम्बन्धीधारणा में क्रान्ति उसी हद तक हो सकती थी, जिस हद तक उसके लिए अनुसन्धान द्वारा निश्चित सामग्री उपलब्ध हुई हो, बहुत पहले ही कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ हो चुकी थीं, जिनके कारण इतिहास की धारणा में एक निर्णयात्मक परिर्वतन सम्भव हुआ। 1831 में लियों नाम के नगर में मज़दूरों का पहला विद्रोह हुआ; 1838 और 1842 के बीच इंग्लैण्ड का चार्टिस्ट आन्दोलन, जो पहला राष्ट्रव्यापी मज़दूर-आन्दोलन था, अपने शिखर पर पहुँच गया। सर्वहारा वर्ग और पूँजीवादी वर्ग का वर्ग-संघर्ष यूरोप के सबसे उन्नत देशों के इतिहास में सामने आया, और उस हद तक सामने आया, जिस हद तक उनमें एक ओर आधुनिक उद्योग का और दूसरी ओर पूँजीवादी वर्ग के नये राजनीतिक प्रभुत्व का विकास हुआ था। तथ्यों ने अधिकाधिक शक्ति के साथ पूँजीवादी अर्थशास्त्रा के उपदेशों को झूठा ठहराया, जिनके अनुसार पूँजी और श्रम के हित एक हैं, और जिनके अनुसार अनियंत्रित होड़ का फल होगा विश्वव्यापी शान्ति और समृद्धि। इन नये तथ्यों की अब और उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, और जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी समाजवाद उनकी सैद्धान्तिक पर अपूर्ण अभिव्यक्ति था, न तो अब उसकी ही उपेक्षा की जा सकती थी। परन्तु इतिहास की पुरानी आदर्शवादी धारणा में - और यह धारणा अभी तक निर्मूल न हुई थी - आर्थिक हितों पर आधारित वर्ग-संघर्षों का, या आर्थिक हितों का, कोई स्थान नहीं था; इस धारणाके अनुसार उत्पादन, तथा सभी आर्थिक सम्बन्ध ''सभ्यता के इतिहास'' के आनुषंगिक और अप्रधान तत्व हैं।
इन नये तथ्यों के कारण समस्त विगत इतिहास की फिर से परीक्षा करना आवश्यक हो गया। और तब यह देखा गया कि आदिम युगों को छोड़कर, समस्तविगत इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है, और समाज के यह संघर्षरत वर्ग सदा अपने युग की उत्पादन तथा विनिमय-प्रणाली से, या एक शब्द में कहें तो, अपने युग की आर्थिक परिस्थितियों से, उत्पन्न हुए हैं; और यह कि समाज का आर्थिक ढाँचाही वस्तुत: वह आधारहै, जिसके ऊपर किसी भी ऐतिहासिक युग की कानूनी और राजनीतिक संस्थाओं की और धार्मिक, दार्शनिक तथा दूसरे विचारों की पूरी इमारत खड़ी की जाती है, और इस आधार को ग्रहण करके ही हम पूरी इमारत को अन्तिम रूप से समझ सकते हैं। हेगेल ने इतिहास को अधिभूतवाद से मुक्त किया, उसने उसे द्वन्द्ववादी रूप दिया, परन्तु इतिहास की उसकी धारणा मूलत: आदर्शवादी थी। आदर्शवाद का अन्तिम आश्रय इतिहास की दार्शनिक धारणा थी, पर जब वह आश्रय भी जाता रहा; अब इतिहास की एक भौतिकवादी विवेचना प्रस्तुत की गयी। अभी तक मनुष्य की चेतना को उसकी सत्ताका आधार माना गया था, पर अब मनुष्य की सत्ता को उसकी चेतना का आधार प्रमाणित करने का मार्ग खुल गया।
इस ज़माने से समाजवाद किसी प्रतिभासम्पन्न मस्तिष्क की आकस्मिक खोज का फल न रह गया। अब वह ऐतिहासिक रूप से विकसित दो-वर्गों, सर्वहारा और पूँजीवादी वर्गों, के संघर्ष का आवश्यक परिणाम समझा जाने लगा। अब उसका उद्देश्य एक यथासम्भव सम्पूर्ण और दोषहीन समाज-व्यवस्था की कल्पना करना न रह गया। जिस ऐतिहासिक-आर्थिक घटनाक्रम से इन वर्गों और उनके विरोध का आवश्यक रूप से जन्म हुआ है, उसकी परीक्षा करना और इस प्रकार से उत्पन्नआर्थिक परिस्थितियों के अन्दर से उन साधनों को ढूँढनिकालना, जिनसे इस संघर्ष का अन्त किया जा सकता है - यह हुआ समाजवाद का नया उद्देश्य। परन्तु इस भौतिकवादी धारणा से, पहले के दिनों के समाजवाद का कोई मेल न था, उसी प्रकार जैसे फ्रांसीसी भौतिकवादियों की प्रकृति सम्बन्धीधारणा का द्वन्द्ववाद तथा आधुनिक प्रकृति-विज्ञान के साथ कोई सामंजस्य न था। पहले के समाजवादियों ने निस्सन्देह अपने काल की पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली और उसके दुष्परिणामों की आलोचना की थी। परन्तु वह उनके कारणों का निर्देश न कर सके, और इसलिए वे उनपर काबू न पा सके। वे उन्हें बुरा समझकर त्याज्य ही ठहरा सकते थे। पुराने समाजवादी पूँजीवाद के अन्तर्गत अनिवार्य, मज़दूर-वर्ग के शोषण की जितनी ही तीव्र निन्दा करते थे, उतना ही वह यह समझाने में, स्पष्ट रूप से यह दिखलाने में असमर्थ रहते थे कि यह शोषण किस बात में है और कैसे उत्पन्न होता है। इसके लिए यह आवश्यक था कि (1)पूँजीवादी उत्पादन-प्रणालीके ऐतिहासिक सम्बन्धोंका निर्देश किया जाये, और यह दिखाया जाये कि एक विशेष ऐतिहासिक युग में उसका उत्पन्न होना अनिवार्य था, और इसीलिए उसका पतन भी अवश्यम्भावी है; और (2) पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के मौलिक स्वरूप को, जो अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी, प्रकट किया जाये। अतिरिक्त मूल्यकी खोज से यह पूरी हो गयी। यह दिखाया गया कि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली और उसके अन्तर्गत होनेवाले मज़दूर के शोषण का आधार यह है कि मज़दूर की मुफ़्तकी मेहनत से जिस मूल्य की सृष्टि होती है, मालिक उसे हड़प लेता है। और अगर पूँजीपति अपने मज़दूर की श्रम-शक्ति को, बाज़ारमेंबिकनेवाले माल के रूप में पूरा दाम देकर ख़रीदता है, तो भी वह उससे, जितना वह उसपर ख़र्च करता है, उससे अधिक मूल्य निकाल लेता है और अन्तत: इस अतिरिक्तमूल्य से ही मूल्यों के वे परिमाण बनते हैं, जिनसे धनी वर्गों के हाथ में एक निरन्तर बढ़ती हुई पूँजी की राशि एकत्रहोती है। पूँजीवादी उत्पादन, और पूँजी के उत्पादन का स्रोत क्या है, यह स्पष्ट हो गया।
इतिहास की भौतिकवादी धारणा, और अतिरिक्त मूल्य के द्वारा पूँजीवादी उत्पादन के रहस्य का उद्घाटन -इन दो महानआविष्कारों के लिए हम मार्क्सके आभारी हैं। इन आविष्कारों के फलस्वरूप समाजवाद एक विज्ञान बन गया। अब इसके बाद जो काम था, वह यह कि उसके सभी ब्योरों और सम्बन्धोंको निश्चित किया जाए।
-फ्रेडरिक एंगेल्स (समाजवाद: काल्पनिक और वैज्ञानिक, 1880)
* विज्ञान के विकास के अलेक्जेंड्रियन काल में ई.पू.तीसरी शताब्दी से ईसा की सातवीं शताब्दी तक का समय लिया जाता है। इसका नाम मिस्र के नगर,अलेक्जेंड्रिया पर पड़ा है,जो उस ज़माने में अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक आदान-प्रदान का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था। अलेक्जेंड्रियन काम में गणित (यूक्लीड और आर्कमेडीज),भूगोल,खगोलशास्त्र,शरीर-रचना विज्ञान और शरीर-विज्ञान आदि का बहुत काफी विकास हुआ था। - सं.
↧
स्वगत
स्वगत (एक)
कभी-कभी ऐसा होता है कि
तुम एकदम अकेले छोड़ दिये जाते हो
सोचने के कारण
या सोचने के लिए
कठिन और व्यस्त दिनों के ऐन बीचो-बीच।
लपटों से उठते है बिम्ब
और फिर लपटों में ही समा जाते हैं।
स्मृति-छायाएँ नाचती हैं निर्वसना
स्वप्नों के लिए नहीं खुलता
कहीं कोई दरवाज़ा ।
हवा एकदम भारी और उदास होती है।
आत्मा का कोई हिस्सा
राख में बदलता रहता है।
तुम्हारे रचे चरित्र चीख़ते हैं।
घटनाएँ-स्थितियाँ अपने विपरीत में
बदल जाती हैं।
तमाम अनुबन्ध्ा
आग के हवाले कर दिये जाते हैं।
प्रार्थनाएँ पास नहीं होतीं।
पुनर्विचार याचिकाओं का
प्रावधान नहीं होता।
मंच पर नीम उजाले में
एक के बाद एक उठते जाते हैं काले पर्दे
और गहराइयों से निकलकार सामने आती हैं
कभी तुम्हारी ग़लतियाँ
तो कभी ग़लतफ़हमियाँ।
राख की एक ढेरी पर
चढ़ते जाते हो तुम हाँफते हुए
और घुटने-घुटने तक धँसते हुए
और फिर थककर बैठ जाते हो।
लेकिन तुम्हारे आँसू चुप रहते हैं
और हथेलियाँ गर्म।
हृदय धड़कता रहता है
और होंठ थरथराते हैं।
आग अपने पीछे
एक काला रेगिस्तान छोड़
किस दिशा में आगे बढ़ गयी है,
तुम जानते की कोशिश करते हो।
सहसा तुम्हें लगता है
कोई आवाज़ आ रही है
उड़-उड़कर,रूक-रूक कर।
शायद वायलिन पर कोई गहन विचार
और सघन उदासी भरी धुन है,
या फिर यह रात की अपनी आवाज़ है।
फिर सन्नाटे में कहीं
गिटार झनझना उठता है
तबले की उन्मत्त थापों के साथ।
किधर से आ रही है हवा
इन आवाज़ों को ढोती हुई,
तुम भाँपने की कोशिश करते हो।
दरअसल जब तुम्हें लग रहा था
कि तुम कुछ नहीं सोच पा रहे थे,
तब फ़ैसलाकुन ढंग से
कोई नतीजा,या कोई नया विचार
तुम्हारे भीतर पक रहा था,
एक त्रासदी भरे कालखण्ड का
समाहार निष्कर्ष तक पहुँच रहा था
और कोई नयी परियोजना
जन्म ले रही थी।
-शशि प्रकाश (नवम्बर,1995)
स्वगत (दो)
(2001 में लिये गये कुछ नोट्स
एक उदास बारिश में जीवन की ऊष्मागतिकी)
बॉयलरों में प्रतीक्षारत था
तारकोल,
आग राख की नींद सो रही थी।
रक्त जैसी रासायनिक संरचना नहीं
फाँसी के फन्दे जैसी
बुनावट थी विचारों की
और भले लोग
तोता कुतरे अमरूद की तरह
डाल से लटक रहे थे।
कुछ यूँ हुई थी एक नयी शताब्दी की
इतिहास में दर्ज़ होने लायक़ शुरुआत
कि अधिकांश मान्य धारणाएँ और परिभाषाएँ
सन्देह के दायरे में आ गयी थीं
विचारकों की दुनिया में
जिसे निर्लज्जता माना जाये।
मसलन,सुभाषित बोलने वाले
कला-साहित्य के मनस्वी कालपुरुष
आपराधिक पूँजी से प्रकाशित
एक अख़बार के सम्पादक बन जा बैठे थे
अत्याधुनिक,
डरावनी शानो-शौक़त वाले
सम्पादकीय कक्ष में,
अपनी चिलमची और काव्यशास्त्र की सिद्धगुटिका
किसी बौने तोताचश्म को सौंपने के बाद
और नयी भरती के लिए
उन कवियों का बायोडाटा देख रहे थे
जिनकी मानवीय संवेदना
बेहद सूक्ष्म-सघन मानी जाती थी
और नेपथ्य में बज रहा था कभी
राग जैजैवंती तो कभी तिलक कामोद।
भागमभाग,भुखमरी,सस्ती शराबों,
अपने सस्ते चुम्बनों के साथ प्रस्तुत कस्बाई लड़कियों,
कटते जंगलों,विस्थापनों,जादुई तकनीकों,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचरित
गलदश्रु भावुकता और बर्बरता और रुग्ण ऐन्द्रिकता
के बीच विचार दलालों की भूमिका में थे
और भाषा
छिनालपन की तमाम हदें पार कर चुकी थी।
एक शब्द - निरुपायता
पूरे ब्रह्माण्ड का भ्रमण कर रहा था
और आकाशवाणी हो रही थी कि
जो भी है,उसे स्वीकार करें सर्वजन
अपनी नियति या सौभाग्य मानकर।
और यह सब कुछ तुम भी देख रहे थे
लेकिन सदियों पुराने अखरोट के
एक वृक्ष की तरह नहीं,
झुण्ड से अलग कर दिये गये
बूढ़े भेड़िये की तरह भी नहीं,
बल्कि सफ़ेदी के विस्तार में
जीते जिद्दी एकाकी ध्रुवीय भालू की तरह।
पूर्वजों द्वारा सौंपी गयी रस्सी से बँधे
ईमानदार,कर्त्तव्यनिष्ट और बहादुर लोग
लगातार भूसे की दँवरी-मड़ाई कर रहे थे
और नयी फ़सलें खेतों में
देख-रेख की माँग कर रही थीं।
सीलन और सड़ाँध भरे
अँधेरे रास्तों से बाहर आये विचार
परिस्थितियों को
अन्धे छछुँदर की तरह सूँघ रहे थे।
अपने बिलों के द्वार पर बैठे झींगुर
नागरिक आज़ादी और जनवाद के बारे में
चीख़ रहे थे
और पैरों की धमक सुनते ही
भीतर दुबक जा रहे थे।
कविता में जीवन था
चहबच्चे के पानी में पलते पूँछदार शिशु मेढकों के मानिन्द ।
तुम सोचने लगे उन दिनों के बारे में
जब आवारा पत्ते की तरह
उड़ते रहे तुम
इस शहर से उस शहर,
इस ठीहे से उस ठीहे,
अनिद्रा,सूख चुके आँसुओं
और बढ़ती हुई झुर्रियों
और टूट चुके रिश्तों की टीसती यादों के साथ,
लातिनी दुनिया के अनगिन रहस्यों
और पुरातन अफ्रीकी योद्धा के
जादुई काले मुखौटे के साथ।
मुहाने तक पहुँचने की ज़िद के साथ
तुम नदी की धारा के साथ तैरते रहे
चीखती गंगाचिल्लियों,कूजते कलहंसों
और ध्यानमग्न बगुलों को
पीछे छोड़ते हुए।
मँडराते रहते थे तुम्हारे आस-पास
पनकुकरी,मछरंगा,कौडि़ल्ला,कचबचिया,फुदकी
और बचपन की जान-पहचान वाले
तमाम जलपक्षी
लेकिन कुछ घण्टे या ज्यादा से ज्यादा
दिन भर के लिए ही
वे रहते थे तुम्हारे साथ।
मुहाने के क़रीब जा पहुँचे थे तुम
चिग्घाड़ते सागर से बस कुछ ही मील दूर
और सोचा मज़े के साथ
अपनी आवारगी को बचा ले जाने की
सफलता के बारे में,
प्रकृत्ति और जीवन और स्त्रियों के
रहस्यों के बारे में
और उन बीहर वनस्पतियों के बारे में
जिनके पत्तों को पीला कर पाने में
दुनिया के तमाम हर्बिसाइड्स नाकाम रहे।
लगभग असम्भव होते जा रहे
हालात से कहीं अधिक,
तब तुम सोच रहे थे
अपनी छोटी-छोटी सफलताओं के बारे में
और यह कि
दुनिया देख घर बैठे लोगों ने
भले ही तुम्हें अकेला करने की
बारहों कोशिशें कीं,
ज़िन्दगी ने कभी तुम्हें नाशुक्रा नहीं माना।
तुम सोच रहे थे कि आकस्मिक
तुम्हारी मृत्यु शान्ति और राहत भरी होगी
कि सहसा एक कुटिल जाल ने
तुम्हें लपेटा और किनारे ला पटका।
एक-दूसरे की आत्माओं को
मृत्युदण्ड दे चुके
विद्वान न्यायमूर्तियों की एक बेंच ने
तुम्हारे जटिल मुकदमे को
चुटकी बजाते सुलझाया
और तुम्हें एक अन्धी सुरंग में
आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया ।
अब तुम्हारे पास सोचने को समय था बहुत कुछ के बारे में,
मसलन,जीवन की वास्तविकता के बारे में
अविश्वासके बारे में,
मौसम की भविष्यवाणियों की अनिश्चितता के बीच
बनायी गयी नयी यात्राओं की योजनाओं के बारे में,
धूमिल-धूसर क्षितिज से परे रोशनी,
धूप में सँवलायी जि़न्दगी,
अनजान द्वीपों के ख़ुशदिल और दिलेर लोगों,
जीवन्तता से सराबोर सस्ती सरायों
और अधिशेष निचोड़ने के नये-नये तौर-तरीकों
और मनुष्यता की न्यूनतम शर्तों को
खो देने वाले लोगों के बारे में।
तुम सोचते रहे
और नदियों के हर घुमाव
तुम्हें याद आते रहे।
तरह-तरह की वनस्पतियाँ
छोटे-छोटे फूलों वाली घास,
संगमरमर की चट्टानों की दरारों में उगी
जिजीविषा जैसी झाड़ियाँ,
क्षितिज तक फैले
निश्चल रेवड़ जैसे जंगल,
बीहड़ मैदानों के खड्ड-खाई भरे विस्तार,
बोझिल और घिसी-पिटी,
भयानक और असह्य कस्बाई कूपमण्डूकी ज़िन्दगी
के बीच पलती निर्मल भावनाएँ और सशक्त कल्पनाएँ,
अकथ दु:खों के बीच भी
हर्ष से हुमकने-छलकने की क्षमता रखने वाली स्त्रियाँ,
मज़बूत इरादों वाले बुद्धू बूढ़े
और नवें आसमान तक उड़ने का
मंसूबा बाँधने वाले नौजवान
तुम्हें याद आते रहे।
स्मृतियाँ तुम्हारे ऊपर
जादुई उपहारों की बारिश करती रहीं
और धूल-धूसरित भोर में अप्रत्याशित
तुमने अपने को खुले आसमान के नीचे पाया
जब तारे बुझने को थे।
तुम मुक्त थे
गगनभेदी तुमुल हाहाकार के बीच
और तुमने सहसा एक आविष्कार किया।
तुमने पाया कि
तमाम पुरातन और नूतन बुराइयों के बावजूद,
मेहनतकश और ईमानदार निश्छल लोगों,
लगातार चकित करती और चुनौती देती
पर्वत-श्रृंखलाओं,सदानीरा नदियों और
सागरों की सुदीर्घ तटरेखा सहित
इस देश को
पृथ्वी के एक बेशकीमती टुकड़े के रूप में
तुम वाक़ई बहुत प्यार करते हो
और इसके भविष्य के बारे में
कई तरह से,कई रूपों में
लगातार सोचते रहते हो।
तुमने जाना कि
अतीत जब तक सोता रहा
भविष्य मुँह चिढ़ाता रहा।
तुमने यह जाना कि
अतीत के कारण हम जीते हैं
और अतीत के करण ही खत्म हो जाते हैं
जैसा कि गोएठे ने कहा था
लेकिन एक नयी शुरूआत के लिए
ज्यादा महत्तवपूर्ण थी गोएठे की ही यह बात
कि एक नयी सच्चाई के लिए एक पुराने भ्रम से
ख़तरनाक कुछ भी नहीं होता।
सपने अब आतुर थे
आलोचनात्मक विवेक के सहारे
भविष्य का पूर्वानुमान बनने के लिए।
दुनिया के गर्म प्रदेशों में
दीवानगी दुनियादारी का ज़हर चूस रही थी
अहसासों में सादगी,
विचारों में मौलिकता,
समर-संकल्पों में निर्णायकता,
प्रतिबद्धता में अटूटता
और प्यार में ईमानदारी की वापसी हो रही थी
और जीवितों की एक छोटी-सी दुनिया
अपने कायाकल्प के लिए
आतुर हो रही थी
अब तुम सोच रहे थे
रात में सफे़द कौंधों और फेनिल लपटों वाले
महासागरों,
रहस्यपूर्ण द्वीपों,उकसाते पर्वतों
और जिज्ञासा जगाते
विराट समतल प्रदेशों के बारे में
और समुद्री शैवाल जैसे
जीवन के आदिम स्रोतों के बारे में
और आने वाले समय के मानचित्र के बारे में।
यूँ तो तमाम भौतिक वस्तुओं की
रहस्यमय गतिविधियों को
पहले भी कभी तुमने
बहते पानी की तली में पड़े
उस निश्चल पत्थ्ार की तरह नहीं देखा था
जिसे शताब्दियों तक बहाव ज़्यादा से ज्यादा
चिकना बनाता रहा।
कभी चक्कों की तरह तो कभी पंखों की तरह गतिमान
तुम चीज़ों की छवियाँ आँकते रहे थे।
पर अब तुम सागर की सर्पिल अग्रगामी लहरों की तरह,
आगे बढ़ते हुए,
एक वर्तुलाकार बवण्डर की तरह
ऊपर उठते हुए,
चीज़ों तक पहुँच रहे थे
और उनके अन्दरूनी द्वन्द्वों का
अध्ययन कर रहे थे।
तुम्हें हँसी आयी
ठूँठों की सभा में कभी प्रस्तुत किये गये
अपने एकायामी विचारों
और रूमानी आह्वानों को याद करके
तुम अब समय-समय पर ऊफन पड़ने वाली
अपनी शिशुवत क्रूरता,
बेहरम लोगों पर की गयी प्यार की बारिश
विरक्तियों के अतिरेक
और जान-बूझकर छले जाने की
अपनी आदतों को भी
एक हद तक समझ पा रहे थे
और तुम्हारी सारी सरगर्मियों का दायरा
एक नया दहनपात्र बन रहा था
जिसमें उबलते रसायन से
कोई नया संश्लिष्ट यौगिक ढलने वाला था
किसी सुनिश्चित योजना के साँचे में।
यह सबकुछ हो रहा था तुम्हारे साथ
और उधर दुनिया लगातार बदलती हुई
कुरुपता-विरुपता के चरम तक पहुँच रही थी
और उसके चलने के तौर-तरीके भी
जटिलतम-कुटिलतम हो चुके थे।
दिशा है सामने एक धुँधली पथरेखा की तरह
और लगातार स्पष्ट होती दृष्टि भी।
चीज़ों को इस हद तक पहचाना जा सकता है
कि आशाओं का स्रोत अक्षय रहे
लेकिन फिर भी बहुतेरी समस्याएँ हैं
नित नयी आती हुई और कुछ अतीत की विरासत भी,
कि नया अभियान नहीं बन पा रहा है ऊर्जस्वी,गतिमान।
अभी भी आस-पास हैं झूठे कमज़ोर संकल्प
और खोखले वायदे,
और अविश्वास,
और पुराने मताग्रह और पुरानी आदतें,
और भ्रमित करने वाले अप्रत्याशित बदलाव भी,
जो तुम्हें लगभग अकेला कर देती हैं
और भीषण तनाव पैदा करती हैं तुम्हारे भीतर,
ज्यों धनुष की प्रत्यंचा की तरह
खिंच गयी हो मस्तिष्क की एक-एक शिरा।
तुम लौटते हो फिर-फिर
अपने एकान्त,उदासियों,अनिद्रा भरी रातों
और घुटन भरे अमूर्तनों के पास,
लेकिन गुफा में घुसते एकाकी योगी की तरह नहीं
बल्कि अपने खाली डोलों को लेकर
कुएँ में उतरती उस रहट की तरह
जो पानी लेकर ऊपर आती है
और डोलों को चुण्डे में उलट देती है।
मानचित्र तैयार है लगभग यात्रा-पथ का,
लेकिन कड़वी पराजयों से उपजी दार्शनिकताओं,
अतृप्तियों-अधूरेपन से जन्मी विकृतियों,
पुरातन और नूतन कूपमण्डूकताओं,
आसमानी आभा वाली आध्यात्मिक वंचनाओं,
शयनकक्षों में रखी गयी
पिस्तौलों और विष के प्यालों से भरे
हमारे इस विचित्र विकट समय में
चीजें फिर भी काफ़ी कठिन हैं।
चन्द राहत या सुकून के दिन आते भी हैं
तो देखते-देखते यूँ बीत जाते हैं
जैसे वीरान खेतों के बीच से
भागती नीलगायों का एक झुण्ड गुज़र जाये।
पंखों,चमड़ों,हड्डियों,पत्तियों,चीथड़ों,मल-मूत्र,
टूटे हुए खिलौनों और तमाम अल्लम-गल्लम चीज़ों से
भरी कूड़ा-करकट जैसी ज़िन्दगी
सड़ती-गलती रही इस दौरान लगातार
कुछ ज़हरीले कीड़े-मकोड़ों के साथ ही
नये-नये पोषक तत्त्व भी पैदा करती हुई।
और हरबा-हथियार एवं रसद के जुगाड़,
रूटीनी कवायद,पूर्वाभ्यास
और हर अनुमानित चुनौती पर विचार जैसी
भावी सुदीर्घ और निर्णायक अभियान की
तनाव भरी तैयारियों के बीच
तुम उतरते हो फिर-फिर
अपने अकेलेपन के कुएँ में थके हुए
खाली डोलों के साथ
बाहर आते हो चीज़ों की ज़्यादा गहरी समझ के
साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सघन-सान्द्र
यह अनुभूति लेकर कि
इस बार फै़सलाकुन होकर निकलना है हमें
नयी बीहड़ लम्बी यात्रा पर
और जीवन को ही ढल जाना है
एक सुदीर्घ 'पोज़ीशनल वारफ़ेयर'के रूप में।
एक बार फिर वह पुरातन आकांक्षा
पुनर्नवा और दुर्निवार बनकर
आती है तुम्हारे पास
कि मुक्तिदायी विचारों को
सबसे पहले,और भरपूर शक्ति
और रचनात्मकता के साथ,
और निरन्तर बहुविध तरीकों से,
उन मनुष्यों तक पहुँचाया जाना चाहिए
जिनके बूते मनुष्यता बची हुई है
लेकिन जिनसे छीन लिया गया है
मनुष्यों जैसा जीवन
और जिनके कल्पनालोक की मुक्ति ज़रूरी है
एक नयी शुरूआत को परवान चढ़ाने के लिए।
ताक़त के खिलाफ़ उन्हें ही साथ लेना होगा
जिनके पास नहीं होती कोई ताक़त
लेकिन एकजुट,और विचारों से लैस होकर
जो बन जाते हैं जड़ और चेतन जगत की
सबसे बड़ी ताक़त।
अनुर्वरता के रौरव रोर के बीच
बिना खिड़कियों-रोशनदानों वाले घरों के
बन्द दरवाज़ों की दरारों से
रिसकर बाहर आ रही है।
प्रसव-वेदना की व्यग्र चीखें।
निश्चय ही,
इस सदी के बीतने से पहले,
शायद काफ़ी पहले,
आकाश को मिल जायेगा उसका अपहृत नीलापन,
इन्द्रधनुष को उसके चुरा लिये गये रंग,
अनुभूतियों को चिरन्तन सुन्दरता,
प्यार को ताज़गी,
विचारों को मानवीय गरिमा,
और भावनाओं को उद्दाम संवेग
और फिर पूरी पृथ्वी चल पड़ेगी
एक नीय आकाशगंगा में रहने के लिए।
वह दिन जब निकट होगा
दुष्टता के उग आयेंगे चींटों जैसे पंख।
तब जो जीवितों की दुनिया होगी,
याद करेगी पीढ़ियों,घिसे हुए आदिम जूतों,
धीरज,रक्त,अपमानजनक पराजयों
और तमाम-तमाम दूसरी चीज़ों के साथ
धरती के गर्भ में
खनिज और खाद बनकर
निश्चल पड़े पूर्वजों को
भरपूर समझदारी और प्यार के साथ।
और हाँ,इन्सानी चर्बी से जल रहे
दीयों की रोशनी में
चर्मपत्रों पर लिखे गये
इतिहास के अन्त और महावृत्तान्तों के विसर्जन के
अभिलेख सुरक्षित रखने होंगे
ताकि आने वाले समय में जाना जा सके
कि एक समय था
जब निराशा इस क़दर गहरी थी।
-शशि प्रकाश (26-29सितम्बर,2005)
↧
↧
अस्तित्व और चेतना
… अत: बात यह है कि निश्चित व्यक्ति,जो उत्पादकता की दृष्टि से निश्चित ढंग से सक्रिय है,निश्चित सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों में प्रवेश करते हैं। इन्द्रियानुभविक पर्यलोकन के लिए यह आवश्यक है कि वह हर अलग-अलग मामले में अनुभव के आधार पर तथा किसी रहस्यीकरण और परिकल्पना के बिना उत्पादन के साथ सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे के सम्बन्ध को सामने लाये। सामाजिक ढाँचा तथा राज्य निश्चित व्यक्तियों की जीवन-प्रक्रिया में से निरन्तर विकसित होते आ रहे हैं,परंतु व्यक्तियों की जीवन-प्रक्रिया से,उस तरह से नहीं जैसे वे उनकी स्वयं की या दूसरों की कल्पना में प्रकट हो सकते हैं,बल्कि जैसे कि वे वास्तव मेंहैं,भौतिक उत्पादन करते हैं और उन सुनिश्चित भौतिक सीमाओं,पूर्वमान्यताओं और स्थितियों के अन्तर्गत क्रियाशील होते हैं जो उनकी इच्छा से स्वतंत्र हैं।
विचारों का,संप्रत्ययों का,चेतना का उत्पादन आरम्भ में लोगों के भौतिक क्रियाकलाप और भौतिक संसर्ग से,वास्तविक जीवन की भाषा से प्रत्यक्षतया गुँथा-बुना होता है। लोगों की संकल्पना,चिन्तन और मानसिक संसर्ग इस मंजिल पर उनके भौतिक आचरण के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। यही बात मानसिक उत्पादन पर लागू होती है जैसा कि किसी जनता की राजनीति,क़ानूनों,नैतिकता,धर्म,तत्वमीमांसा आदि की भाषा में अभिव्यक्त होता है। अपने संप्रत्ययों,विचारों आदि के उत्पादक मनुष्य हैं - वास्तविक सक्रिय मनुष्य,उस रूप में,जिस रूप में वे अपनी उत्पादक शक्तियों के तथा इनके समरूप संसर्ग के निश्चित विकास द्वारा,उनके दूरतम रूपों द्वारा अनुकूलित होते हैं। चेतना चेतन अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती,तथा मनुष्य का अस्तित्व उसकी वास्तविक जीवन-प्रक्रिया होता है। यदि समग्र विचारधारा में मनुष्य और उनकी परिस्थितियाँ camera obscuraकी तरह उलटी नज़र आती हैं तो यह घटना उनकी ऐतिहासिक जीवन-प्रक्रिया से उसीतरह उत्पन्न होती है जिसप्रकार दृष्टिपटल पर वस्तुओं का प्रतिलोमन उनकी शारीरिक जीवन-प्रक्रिया के कारण होता है।
जर्मन दर्शन के,जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरता है,ठीक विपरीत यहाँ हम पृथ्वी से स्वर्ग पर आरोहण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य,जो कहते हैं,कल्पना करते हैं,अनुमान लगाते हैं,हम उसे आधार बनाकर अग्रसर नहीं होते,न हम लोंगों को उस रूप में आधार बनाकर अग्रसर होते हैं,जिस रूप में उनका वर्णन किया जाता है,उनके बारे में सोचा जाता है,उनकी कल्पना की जाती है,उनके बारे में अनुमान लगाया जाता है,ताकि वास्तविक मनुष्यों तक पहुँचा जा सके। हम वास्तविक,सक्रिय मनुष्यों से प्रस्थान करते हैं और उनकी वास्तविक जीवन-प्रक्रिया के आधार पर इस जीवन-प्रक्रिया के विचारधारात्मक प्रतिवर्तों के विकास ओर उसकी प्रतिध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं। मानव मस्तिष्क में बनने वाले छायाभास भी,अनिवार्यत: उनकी उस भौतिक जीवन-प्रक्रिया के उदात्तीकृतरूप हैं जो अनुभव द्वारा परखी जा सकती है और भौतिक पूर्वाधारों से बँधी हुई है। इसतरह,नैतिकता,धर्म,तत्वमीमांसा,बाकी सारी विचारधारा तथा चेतना के उनके तदनुरूपी रूप स्वतंत्र नहीं हो सकते। उनका कोई इतिहास,कोई विकास नहीं;परंतु मनुष्य अपने भौतिक उत्पादन और अपने भौतिक संसर्ग का विकास करते हुए अपने वास्तविक अस्तित्व के साथ अपने चिन्तन तथा अपने चिन्तन के उत्पादों को भी बदलते रहते हैं। जीवन चेतना द्वारा निर्धारित नहीं होता,अपितु चेतना जीवन द्वारा निर्धारित होती है। अप्रोच की पहली पद्धति में चेतना एक सजीव व्यक्ति के रूप में प्रस्थान-बिन्दु है;दूसरी विधि में यह वास्तविक सजीव व्यक्ति स्वयं हैं,जैसे कि वे असली जीवन में होते हैं और चेतना को मात्र उनकीचेतना के रूप में लिया गया है।
अप्रोच की यह पद्धति पूर्वाधारों से वंचित नहीं है। वह वास्तविक पूर्वाधारों से प्रस्थान करती है और उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। उसके पूर्वाधार मनुष्य हैं,किसी अतिकाल्पनिक अलग-थलग अवस्था में या अमूर्त परिभाषा में नहीं,बल्कि निश्चित स्थितियों में होने वाले अपने वास्तविक,आनुभविक ढंग से बोधगम्य विकास की प्रक्रिया में शामिल मनुष्य हैं। जैसे ही इस सक्रिय जीवन-प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है,इतिहास मृत तथ्यों का संग्रह नहीं रह जाता,जैसा कि अनुभववादी उसे बना देते हैं (जो स्वयं अब भी अमूर्त हैं),और वह कल्पित कर्ताओं की कल्पित गतिविधि भी नहीं रह जाता,जिस रूप में भाववादी उसे प्रस्तुत करते हैं।
जहाँ काल्पनिक चिन्तन का अन्त होता है - वास्तविक जीवन में - वहाँ से वास्तविक,सकारात्मक विज्ञान की शुरुआत होती है: जो व्यावहारिक क्रियाकलाप का,मनुष्यों के विकास की व्यावहारिक प्रक्रिया का निरूपण करता है। चेतना के बारे में खोखली बातें बन्द हो जाती हैं,तथा वास्तविक ज्ञान उसका स्थान ले लेता है। जब यथार्थ का चित्रण किया जाता है,तो दर्शन,ज्ञान की स्वतंत्र शाखा के रूप में अपने अस्तित्व का माध्यम खो देता है। ज्यादा से ज्यादा से यह हो सकता है कि इसका स्थान मनुष्यों के ऐतिहासिक विकास के प्रेक्षणों से नि:सृत अमूर्तन,सर्वाधिक सामान्य निष्कर्षों का समाहार ले ले। वास्तविक इतिहास से अलग करके देखें तो वैसे भी इन अमूर्तनों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। वे तो ऐतिहासिक सामग्री को व्यस्थित करने का काम सुगम बनाने,उसकी पृथक परतों के क्रम को लक्षित करने का ही काम दे सकती हैं। परंतु वे इतिहास के युगों को साफ-सुथरे ढंग से सँवारने के लिए कोई नुस्खा या योजनाबंदी प्रस्तुत नहीं करतीं,जैसाकि दर्शन करता है। इसके विपरीत हमारी कठिनाइयाँ ठीक उस समय शुरू होती है जब हम अपनी ऐतिहासिक सामग्री का,वह चाहे बीते युग की हों या वर्तमान की,प्रेक्षण करना तथा उसे क्रमबद्ध करना - यानी वास्तविक चित्रण करना - आरम्भ करते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करना उन पूर्वाधारों पर निर्भर है,जिन्हें यहाँ बताना सर्वथा असम्भव है,लेकिन जिन्हें हर युग की मनुष्यों की वास्तविक जीवन-प्रक्रिया तथा कार्यक्रलाप का अध्ययन ही प्रकाश में ला सकता है।
- कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स (जर्मन विचारधारा,1846)
↧
'पहल' का अगस्त अंक
↧
'पहल'का सितम्बर अंक
↧
उत्पादन-प्रणाली सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन-प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है
अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित सम्बन्धों में बँधते हैं,जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के ये सम्बन्ध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजि़ल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन सम्बन्धों का पूर्ण योग ही समाज का आर्थिक ढाँचा है - वह असली बुनियाद है,जिस पर कानून और राजनीति का ऊपरी ढाँचा खड़ा होता है और जिसके अनुकूल ही सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक,राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती,बल्कि उलटे उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अपने विकास की एक ख़ास मंजिल पर पहुँच कर समाज की भौतिक उत्पादन शक्तियाँ तत्कालीन उत्पादन सम्बन्धों से,या - उसी चीज़ को क़ानूनी शब्दावली में यों कहा जा सकता है - उन सम्पत्ति सम्बन्धों से टकराती हैं,जिनके अन्तर्गत वे उस समय तक काम करती होती हैं। ये सम्बन्ध उत्पादन शक्तियों के विकास के अनुरूप न रहकर उनके लिए बेड़ियाँ बन जाते हैं। तब सामाजिक क्रांति का युग शुरू होता है। आर्थिक बुनियाद के बदलने के साथ समस्त बृहदाकार ऊपरी ढाँचा भी कमोबेश तेजी से बदल जाता है। ऐसे रुपान्तरणों पर विचार करते हुए एक भेद हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक ओर तो,उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों का भौतिक रुपान्तरण है,जिसे प्रकृति विज्ञान की अचूकता के साथ निर्धारित किया जा सकता है। दूसरी ओर वे कानूनी,राजनीतिक,धार्मिक,सौन्दर्यबोधात्मक या दार्शनिक,संक्षेप में,विचारधारात्मक रूप हैं,जिनके दायरे में मनुष्य इस टक्कर के प्रति सचेत होते हैं और उससे निपटते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय इस बात पर नहीं निर्भर होती है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है,उसी तरह हम ऐसे रुपान्तरण के युग के बारे में स्वयं उस युग की चेतना के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते। इसके विपरीत भौतिक जीवन के अन्तरविरोधों के आधार पर ही,समाज की उत्पादन शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धों की मौजूदा टक्कर के आधार पर ही इस चेतना की व्याख्या की जानी चाहिए। कोई भी समाज-व्यवस्था तब तक ख़त्म नहीं होती,जबतक उसके अन्दर तमाम उत्पादन शक्तियाँ,जिनके लिए उसमें जगह है,विकसित नहीं हो जातीं और नये,उच्चतर उत्पादन सम्बन्धों का आर्विभाव तबतक नहीं होता,जबतक कि उनके अस्तित्व की भौतिक परिस्थितियाँ पुराने समाज के गर्भ में ही पुष्ट नहीं हो चुकतीं। इसलिए मानवजाति अपने लिए हमेशा केवल ऐसे ही कार्यभार निर्धारित करती है,जिन्हें वह सम्पन्न कर सकती है। कारण यह है और मामले को ग़ौर से देखने पर हमेशा हम यही पायेंगे कि स्वयं कार्यभार केवल तभी उपस्थित होता है,जब उसे सम्पन्न करने के लिए ज़रूरी भौतिक परिस्थितियाँ पहले से तैयार होती हैं या कम से कम तैयार हो रही होती हैं। मोटे तौर से एशियाई,प्राचीन,सामन्ती एवं आधुनिक,पूँजीवादी उत्पादन प्रणालियाँ समाज की आर्थिक विरचना के अनुक्रमिक युग कही जा सकती है। पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध उत्पादन के सामाजिक प्रक्रिया के अन्तिम वैरभावपूर्ण रूप हैं - व्यक्तिगत वैरभाव के अर्थ में नहीं,वरन् व्यक्तियों के जीवन की सामाजिक अवस्थाओं से उदभूत वैरभाव के अर्थ में। साथ ही पूँजीवादी समाज के गर्भ में विकसित होती हुई उत्पादक शक्तियाँ इस विरोध के हल की भौतिक अवस्थाएँ उत्पन्न करती हैं। अत: इस सामाजिक विरचना के साथ मानव समाज के विकास का प्रागैतिहासिक अध्याय समाप्त हो जाता है।
कार्ल मार्क्स,('राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना के एक प्रयास की भूमिका',1859)
↧
↧
संस्मरण लेखन के बारे में कुछ स्फुट विचार
कविता कृष्णपल्लवी
हिंदी साहित्य् में कुछ वर्षों से संस्मरण खूब लिखे जा रहे हैं। इनमें लेखकगण नौजवानी के दिनों की अपनी आवारागर्दियों के चर्चे करते हैं, शराबनोशी के किस्से बयान करते हैं और लगे हाथों उन प्रतिस्पर्द्धियों की टांग खिंचाई करते हैं जिनसे कुछ हिसाब-किताब चुकता करना होता है।
इन संस्मरणों में संदर्भित देशकाल का सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक परिदृश्य लगभग अनुपस्थित रहता है। पाब्लो नेरूदा, मक्सिम गोर्की, ब्रेष्ट, लूनाचार्स्की, ओदीसियस इलाइतिस, आदि विश्व के कई रचनाकार हैं जिनके संस्मरणात्मक लेखन में उनका पूरा देशकाल प्रामाणिक रूप में उपस्थित दीखता है। आधी सदी पहले के कई भारतीय लेखकों के संस्मरणों में भी उनके समय का सामाजिक-राजनीतिक-साहित्यिक परिदृश्य उपस्थित दीखता है। साथ ही वे अपने व्यक्तित्व की निर्माण-प्रक्रिया और अपनी रचना-प्रक्रिया पर भी वस्तुतपरक ढंग से बातें करते दीखते हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से इन कृतियों को इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूसो अपनी कालजयी कृति 'आत्मस्वीकृतियां'में जितने साहसिक और बेरहम ढंग से स्वयं अपनी चीरफाड़ करते हैं, वह अदभुत है।
राजनीतिक संस्मरणों पर यदि निगाह डालें तो फ्रांज मेहरिंग की कृति 'कार्ल मार्क्स'और क्रुप्स्काया की कृति 'लेनिन' का उदाहरण लिया जा सकता है। ये दोनों कृतियां दो युगनायकों के जीवन के सहज सामान्य मर्मस्पर्शी चित्रों के साथ ही उनके युगों का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करती प्रतीत होती हैं।
हिंदी के लेखक प्राय: महान लेखक के रूप में इतिहास के पन्नों में इन्दराज़ी के लिए संस्मरण लिखते हैं। यह अलग बात है कि कुछ सिफारिशी और 'फेसबुकी'चर्चाओं के बाद ये संस्मरण भुला दिए जाते हैं। साहित्य सुधी पाठकों द्वारा पढ़ा जाना तो दूर, दीमकें तक इन्हें चाटना पसंद नहीं करतीं। 'नॉरसिसस-ग्रंथि'और गुटपरस्ती लेखकों की आम प्रवृत्ति है और कथित वामपंथी लेखक तो इनमें शायद औरों से भी आगे हैं। यदि आप ''उभरती हुई प्रतिभा''के रूप में चर्चित होना चाहते हैं, तो किसी मठाधीश या किसी प्रभावी मण्डल का शरणागत हो जाइए। फिर शायद किसी के संस्मरण में भी आपका नाम आ जाएगा।
जो कथित वामपंथी कवि लेखक हैं, दरअसल विचारधारात्मक-राजनीतिक समझदारी की दृष्टि से उनमें से भी अधिकांश एकदम कंगाल होते हैं। अपने देश के उत्पादन संबंधों और राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचना में हुए और हो रहे बदलावों के बारे में उनकी कोई समझ नहीं होती। विश्व पूंजीवाद की संरचना और कार्यप्रणाली में विगत तीन-चार दशकों में हुए बदलावों के बारे में वे लगभग कुछ नहीं जानते। मार्क्सवाद की शायद ही कोई क्लासिकी कृति उन्होंने कभी पढ़ी हो। ऐसी स्थिति में अनुभव संगत पर्यवेक्षण के आधार पर अपने रचनात्मक लेखन में भी वे अपने समय और समाज का सामाजिक जीवन, सामाजिक अंतर्सम्बंधों, व्यक्तित्वों की बनावट-बुनावट तथा उनके आत्मिक संसार का मात्र आभासी, खण्डित या विरूपित चित्र ही उपस्थित कर पाते हैं। ऐसे लेखक जब संस्मरण लिखते हैं तो अपने देशकाल का चित्र इसलिए नहीं उपस्थित कर पाते क्योंकि उसकी गतिकी को वे समझते ही नहीं। चलते-चलाते 'बाजार उपनिवेशवाद', 'भूमंडलीकरण', 'पुनर्औपनिवेशीकरण'आदि जुमले वे इस्तेमाल करते रहते हैं पर उनकी कोई समझ नहीं होती। मार्क्सवाद और अंबेडकर को पढ़े बिना वे दोनों की खिचड़ी पकाने की विधि सुझाते हैं। कभी वे 'आइडेंटिटी पॉलिटिक्सं'और 'सबऑल्टर्न'इतिहास लेखन के साथ, तो कभी उत्तर आधुनिकता के साथ मार्क्सवाद का संगम कराते हैं। कुछ युवा लेखक हैं जो पढ़-लिख कर ऐसा करते हैं। उनसे तो बहस हो सकती है,पर कविता-कहानी लिखने वाले ज्यादातर लेखक ऐसे हैं जो बस कुछ शब्द और जुमले बोलते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। ऐसे लोग जब संस्मरण लिखते हैं, तो उनमें उनके समय का इतिहास या तो अनुपस्थित रहता है या बलात्कृत, क्षत-विक्षत रूप में उपस्थित रहता है।
कुछ लेखकों के संस्मरणों में अभिशप्त वर्तमान से मुंह मोड़ कर, मनोगतवादी ढंग से, अतीत में गांव में (या कस्बे् में) बिताये गए जीवन के ''शांत मनोरम''दिनों को 'नॉस्टैल्जिक'होकर याद करने की प्रवृत्ति दिखती है...वे आम के बाग, वह पीपल के पेड़ पर चढ़कर तालाब में छलांग लगाना... वगैरह-वगैरह। ऐसे संस्मरण लिखने वाले प्राय: सवर्ण लेखक होते हैं, जिनके बाप-दादे ज़मींदार थे। एक दलित उन गांवों को तो दु:स्वप्न की तरह ही याद कर सकता है। एक उजड़ा हुआ किसान, जो भले ही महानगर में आकर उजरती गुलामी कर रहा हो, वह भी शहरी नर्क को अतीत के गांव के नर्क से बेहतर ही मानता है। 'नॉस्टैल्जिक'संस्मरणागत लेखक इस बात को समझता ही नहीं कि अपनी स्वाभाविक गति से पूंजी द्वारा ग्रामीण जीवन के पोर-पोर को भेदा ही जाना था। गांव में पूंजी का वर्चस्व, किसान आबादी का विभेदीकरण, ध्रुवीकरण, सर्वहाराकरण, नगरों की ओर पलायन – यह सब होना ही था। जो अतीत वापस लौट नहीं सकता, उसके लिए विलाप निरर्थक है। सच यह है कि वह अतीत भी वैसा शांत-सुरम्य-सुंदर कदापि नहीं था, जैसा याद करने में लगता है। एक गतिहीन, कूपमण्डूक बर्बरता का स्थान आज एक भूचाली, शातिर आततायीपन ने ले लिया है। इसका विकल्प अतीत में नहीं ढूंढ़ा जा सकता, बल्कि भविष्य में ढूंढ़ा जा सकता है।
हल्के-फुल्के तौर पर कहा जा सकता है कि वर्तमान-व्याकुल, अतीत-शरणागत लेखक जब संस्मरण लिखते हैं तो पार्श्वभूमि में ''जाने कहां गए वो दिन...''या ''कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन...''की धुन बजती रहती है। पार्श्वभूमि में यदि ''जिंदगी के सफर में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते...''या ''मुड़-मुड़ के ना देख, मुड़-मुड़ के...'' की धुन बजती रहती तो बेहतर होता।
सच तो यह है कि हिंदी के जो धोती-कुर्ता छाप, खैनी मलते-खाते लेखक-आलोचक आजकल दिल्ली के महानगरीय जीवन के मजे ले रहे हैं, वे भले ही 'अहा ग्राम्य् जीवन'की रट लगाएं, किसी भी कीमत पर वे गांव में जाकर रहने को तैयार नहीं होंगे। जो लेखक संस्मरणों में अतीत को शरण्य बना रहे हैं, उन्हें यदि उस अतीत में ले जाकर पटक दिया जाए तो वे बिलबिला उठेंगे। दरअसल, अतीत को शरण्य वे बनाते हैं, जो भविष्य को देख-पहचान नहीं पाते, या फिर जिनका वर्तमान सुखी-संतुष्ट होता है कि किसी बेहतर भविष्य के लिए लड़ने के लिए उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती।
↧
साधो, ये मुरदों का गाँव
-कविता कृष्णपल्लवी
पाठ्यपुस्तकों में हम पढ़ते आये हैं,'साहित्य समाज का दर्पण है।'लेकिन समकालीन हिन्दी कविता,कहानी,उपन्यास,नाटक आदि पढ़कर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इनमें आज का भारत और इसके लोग कहीं उपस्थित हैं।
इनमें ज़्यादातर मध्यवर्गीय खाये-अघाये लोगों की यौन रसलीलाएँ और रुग्ण फन्तासियाँ हैं,विदेशी कविताओं की नक़ल पर लिखी गयी सूखे भूसे जैसी या अबूझ पहेलियों जैसी कविताएँ हैं,इतिहास की गति से पीछे छूट चुके अतीत के लिए विलाप है,जनपक्षधरता के नाम पर जनजीवन के काल्पनिक और अप्रामाणिक चित्र हैं और संस्मरणों के नाम पर देश-काल से विच्छिन्न आत्मुग्धता के रेखाचित्र हैं।
यूँ कहने को ज़्यादातर लेखक अपने को वामपंथी ही कहते हैं,लेकिन उनके पास न तो 'जनसंगऊष्मा'है,न ही इतिहास-बोध और वैज्ञानिक विवेक है। इधर-उधर से,पल्लवग्राही तरीके से,कुछ पंजीरी लेकर कोई मार्क्सवाद की ऐसी-तैसी कर रहा है,कोई उत्तरआधुनिकतावाद पर अनर्गल प्रलाप कर रहा है,कोई 'आइडेण्टिटी पॉलिटिक्स'की देगची में मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद का शोरबा पका रहा है तो कोई साहित्य के समाजशास्त्र के नाम पर साहित्यालोचना-सिद्धान्त और समाजशास्त्र की बखिया उघेड़ रहा है। ऐसी वैचारिक कंगाली इतिहास के पन्नों पर शर्मनाक़ कलंकित दिनों के रूप में दर्ज़ रहेगी।
राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में सम्पादक के रूप में बालकृष्ण भट्ट,महावीर प्रसाद दिवेदी,गणेश शंकर विद्यार्थी,माखन लाल चतुर्वेदी,प्रेमचन्द आदि ने रचनाकारों के लिए शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। आज कोई भी 'आँख का अंधा गाँठ का पूरा',जो लिख नहीं सकता,वह जेब से पैसे ख़र्च करके एक पत्रिका निकाल देता है और अपने आप को लघु पत्रिका आन्दोलन का खंभा समझने लगता है। छपास के रोगियों की रचनाओं से उसकी मेज भर जाती है। फिर वह एक बड़ी मेज और बड़ी कुर्सी ख़रीदने फ़र्नीचर की दुकान की ओर भागता है। जो कविता-कहानी नहीं लिख सकता है और पत्रिका भी नहीं निकाल सकता,वह दर्शन,आलोचना-सैद्धान्तिकी और सौन्दर्यशास्त्र की बुनियादी किताबें छुए बिना ही आलोचक बन जाता है।
हिन्दी साहित्य की दुनिया मुख्यत: आत्मतुष्ट कूपमण्डूकों की दुनिया है,यह लिलिपुटियंस की दुनिया है,दरबारी चाटुकारों,गुटबाजों और भोगी-विलासी आवारागर्दों की दुनिया है,ऐसे अवसरवादियों की दुनिया है जो अफसर,प्रोफेसर,पत्रकार,डॉक्टर आदि पेशों में लगे मलाई चाटते हैं और जनता के दु:खों पर गाहे-बगाहे उतना घड़ियाली आँसू बहा लेते हैं,जितना प्रगतिशील का तमगा लेने के लिए ज़रूरी होता है। अवसरवाद भी इतना गंदा और बदबूदार किस्म का है कि पूछिये मत!विद्यानिवास मिश्र के चेले,जनेऊधारी पुरबिहा ब्राह्मण विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं,पर उनका कृपापात्र बनने के लिये कई कथित वामपंथी कवि-लेखक-आलोचक आपको उनके आगे-पीछे घूमते,उनकी कविता को 'महान प्रगतिशील कविता'सिद्ध करते मिल जायेंगे। लीलाधर जगूड़ी वामपंथी कवि हैं (पहाड़ी वामपंथी कवियों के गुट के मान्य सदस्य हैं) पर कभी वे भाजपाई मंत्री को पितातुल्य बता रहे थे और अब उत्तराखंण्ड की कांग्रेसी सरकार की पहाड़ों में नदियों पर बाँध बनाने की विनाशकारी नीति की जमकर वकालत कर रहे हैं। कवि केदारनाथ सिंह मुलायम सिंह के सैफई महोत्सव में पहुँचकर इलाके की प्रगति देखकर भावविभोर हो गये और बोल उठे कि देश की बागडोर यदि 'नेताजी'के हाथों में आ जायेगी तो वो पूरे देश को ऐसा ही धनधान्यपूर्ण बना देंगे। शीला दीक्षित,नीतीश कुमार और दूसरे मुख्यमंत्रियों की सरकारों के खुलेआम आगे-पीछे घूमने वाले या छुपकर लाभ उठाने वाले प्रगतिशीलों की भी कमी नहीं है।
सरकारी और पूँजीपतियों के प्रतिष्ठानों के पुरस्कारों की भरमार हो चली है। दर्ज़नों तो लखटकिया पुरस्कार हैं। पहले एक भारत भवन था,अब एक म.गा.हि.वि.वि. भी है और दर्ज़नों साहित्य और कला के नये प्रतिष्ठान खुल गये हैं। एन.जी.ओ. वाले भी इस धन्धे में उतर आये हैं। अखबार वाले भी उतर आये हैं। अंग्रेजी के कुलीनतावादी तो हिन्दी वालों को अब भी दो कौड़ी का ही मानते हैं,पर हिन्दी वाले तो पद-पीठ-पुरस्कारों के मात्र इतने विस्तार से ही फूले नहीं समा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में सम्मान्य अग्रजों के नाम पर स्थापित पीठों पर एक से एक कूपमण्डूक धंधेबाज विराजमान हैं। कुछ पुरस्कारों के बहाने मास्को-लंदन की सैर कर ले रहे हैं,तो कुछ प्रकाशकों को पटाकर या दूतावासों में टिप्पस भिड़ाकर। कोई इनसे बैर नहीं मोल लेता। ये सभी ख़तरनाक माफिया गिरोह के समान होते हैं। इनके ख़िलाफ़ ज्यों ही कोई चूँ भी बोला,ये सभी आपसी तकरार भूलकर एकजुट हो जाते हैं और उसपर टूट पड़ते हैं,साहित्य-संसार से उसे बहिष्कृत कर देते हैं,उसकी रचनाओं को खारिज कर देते हैं,या उसके ख़िलाफ़ चुप्पी का षड्यंत्र रचने लगते हैं,या फिर अफवाहें फैलाने लगते हैं।
आप पुस्तक मेले में हिन्दी प्रकाशकों के स्टॉलों पर जाइये,मण्डी हाउस,इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर,इण्डिया हैबिटेट सेण्टर,साहित्य अकादमी और विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभगों में जाइये ओर चुपचाप हिन्दी के लेखकों-कवियों को निरखिये-परखिये। उधर एक बूढ़ा कवि लाल मफलर लपेटे एक युवा कवयित्री के पीछे लार टपकाते कुत्ते की तरह भागा जा रहा है। एक मोटा तुंदियल पत्रकार-लेखक एक लेखिका की प्रशंसा करते हुए उसपर गिरा जा रहा है। एक अधेड़ कवयित्री अपनी आधुनिकतावादी कविताओं से अलग छायावादी अदायें दिखा रही है। एक कुलपति,एक अकादमी अध्यक्ष और एक विभागाध्यक्ष के आस-पास लोग मण्डलियाँ बनाये खड़े हैं,उनके चियारे हुए दाँतों की चमक में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं। एक झबरीले बालों वाला कवि अपनी विदेश यात्रा के किस्से सुना रहा है। एक लेखक अपनी रचनाओं की प्रशंसाएँ गिना रहा है। एक नया सम्पादक दौड़ता हुआ माननीयों को अपनी पत्रिका थम्हा रहा है। कुछ माननीय परिचितों को न पहचानते हुए यूँ गज़र रहे हैं मानों भीड़ के सिर पर से तैरते हुए जा रहे हों। कहीं गुज़री हुई शराब की महफिलों की चर्चा हो रही है तो कहीं आगे की योजना बन रही है।
इन लोगों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये ऐसे देश के साहित्यकार हैं,जहाँ शिखरों पर समृद्धि की तमाम चकाचौंध के बावजूद 21 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं,18करोड़ लोग बेघर हैं और 18 करोड़ लोग झुग्गियों या कच्चे घरों में रहते हैं,35करोड़ भारतीयों को अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता है, 50फीसदी बच्चे कुपोषित हैं,75फीसदी माँओं को पोषणयुक्त भोजन नहीं मिलता,सालाना 1.17लाख स्त्रियाँ गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मर जाती हैं और 77फीसदी आबादी रोज़ाना 20 रुपये से भी कम पर जीती हैं(इसमें से 22फीसदी रोज़ाना 11.60रुपये पर,19फीसदी रोज़ाना 11.60 से 15 रुपये के बीच की आमदनी पर गुज़ारा करती है)।मानव विकास सूचकांक और वैश्विक भूख सूचकांक के हिसाब से,बच्चों की मृत्यु दर,भुखमरी और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मामले मेंभारत,अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई बेहद ग़रीब देशों से भी पीछे है। अरबपतियों की कुल दौलत के लिहाज से भारत अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नम्बर पर है,लेकिन दूसरी ओर,बेघरों,कुपोषितों,भूखों और अनपढ़ों की तादाद के लिहाज़ से भी,यह दुनिया में पहले नम्बर पर है। देश की ऊपर की दस फीसदी आबादी के पास कुल परिसम्पत्ति का 85 प्रतिशत इकट्ठा हो गया है,जबकि नीचे की 60 फीसदी आबादी के पास मात्र दो प्रतिशत है। देश में 0.01 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी आबादी पूरे देश की औसत आमदनी से दो सौ गुना अधिक है। ऊपर की तीन फीसदी और नीचे की चालीस फीसदी आबादी की आमदनी के बीच का अन्तर आज साठ गुना हो चुका है।
यह है आज़ादी के बाद के 66 वर्षों के पूँजीवादी विकास का बैलेंसशीट। लोकतंत्र की असलियत यह है कि चुनाव के पाँचसाला प्रहसन और नेताशाही-नौकरशाही पर होने वाले ख़र्च के मामले में भारत विकसित पूँजीवादी देशों से भी आगे है। देश के भीतर और बाहर काले धन का इतना अम्बार संचित है कि उससे पूरी आबादी के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य,नि:शुल्क शिक्षा और आवास का इन्तज़ाम किया जा सकता है। चुनावी वामपंथी मदारियों सहित सभी संसदीय पार्टियों की जनता के साथ खुली गद्दारी की भूमिका साफ़ हो चुकी है। स्थापित ट्रेडयूनियनें कमीशनखोर दलालों के गिरोह से अधिक कुछ भी नहीं है। इस दायरे के बाहर कोई संगठित क्रान्तिकारी विकल्प अभी मौजूद नहीं है। गतिरोध और विपर्यय का दमघोंटू माहौल है। संक्रमण का कठिनतम कालखण्ड है। क्रान्तिकारी संकट यहाँ-वहाँ स्वत:स्फूर्त जनविस्फोटों को दे रहा है,लेकिन क्रान्तिकारी दिशा की सुनिश्चित समझ से लैस किसी पार्टी के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग के संगठित नहीं होने के कारण यह क्रान्तिकारी संकट क्रान्ति का पूर्वाधार नहीं बन पा रहा है।
एक पीड़ादायी,लम्बी,क्रमिक प्रक्रिया से पूँजी भारतीय समाज के पोर-पोर को बेध चुकी है। प्रतिवर्ष पूँजी की मार से करोड़ों किसान कंगाल होकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहाँ झुग्गियों में वे नर्क़ का जीवन बिताते हैं। 95 फीसदी शहरी और ग्रामीण मज़दूर असंगठित हैं,जिनके लिए श्रम क़ानूनों का व्यवहारत: कोई मतलब ही नही है। उत्पादन सम्बन्धों में बदलाव के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक ऊपरी ढाँचे में भी भारी बदलाव आये हैं। पुरानी मध्ययुगीन बर्बरताएँ अभी भी क़ायम हैं,पर नये शासकों की सेवा कर रही हैं। नयी बर्बरताओं ने पुरानी बर्बरताओं के साथ सहमेल क़ायम कर लिया है।
इन सारी सच्चाइयों की इन्दराज़ी साहित्य में कत्तई नहीं हो पा रही है,क्योंकि हमारा साहित्यकार जनता के जीवन और संघर्षों से दूर,बहुत दूर खड़ा है। वह ऐसा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है जो जनता के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात कर चुका है।
दरअसल,हिन्दी के साहित्यकारों का बहुलांश (प्रोफेसर,पत्रकार,अफसर और उच्च आय वाले स्वतंत्र पेशेवर के रूप में) देश के उस 15-20 करोड़ खाते-पीते मध्यवर्ग का हिस्सा बन चुका है,जिसकेलिए तमाम अपार्टमेण्ट्स हैं,शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स हैं,होटल-रिसॉर्ट्स-रेस्टोरेण्ट्स हैं,पचासों किस्म की कारें हैं,बचत-बीमा की स्कीमें हैं तथा खाने-पीने-पहनने-ओढ़ने की महँगी चीज़ों के सैकड़ों विकल्प हैं। साहित्य इनके लिए जनता को मुक्ति के स्वप्न और विचार देने का माध्यम नहीं,बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मतुष्टि का साधन मात्र है।
लेकिन इतिहास की यात्रा पर पूर्ण विराम यहीं नहीं लगने वाला है। समय आयेगा जब जनता इन साहित्यिक जड़वामनों से हिसाब माँगेगी। वह पूछेगी कि वे क्या कर रहे थे जब निराशा,अंधकार और रक्त में जनता की ज़िन्दगी को,उसके स्वप्नों और आकांक्षाओं को डुबो देने की कोशिश की जा रही थी। तब इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। फिर जनता इनपर थूकेगी। उस थूक की ढेरी पर ये बौने लोग मक्खियों के समान अपने पंख फदफदायेंगे।
ये जो पद-पीठ-पुरस्कार हैं,यह जो कथित नाम और प्रतिष्ठा है,तब घोड़े की लीद के समान बेकार सिद्ध होंगे। वर्तमान व्यवस्था में,जैसा कि उरुग्वे के प्रसिद्ध जन-सरोकारी सर्जकएदुआर्दो गालिआनो ने एक भाषण में कहा था,''यह सत्तातंत्र है जो हमेशा तय करता है कि मानवता के नाम पर किसे याद रखा जाये और किसे भुला दिया जाये।''फिर भी न गोर्की,लूशुन और नाज़िम हिकमत को भुलाया जा सका है,न प्रेमचंद,राहुल और मुक्तिबोध को। जनता के जीवन,संघर्ष और स्वप्नों के भागीदार सृजनकर्मियों की धारा संकटग्रस्त और कमज़ोर हो सकती है,पर समाप्त नहीं हो सकती। उसे परम्परा और भविष्य स्वप्नों से ऊर्जा मिलती रहेगी। प्रशस्ति पत्रों,पुरस्कारों,तमगों की उसे दरकार नहीं।
एदुआर्दो गालियानोंने एक जगह लिखा है:''मुझे यह भय काफ़ी सताता है कि हम सभी स्मृतिलोप का शिकार हो रहे हैं। मैं मानवीय इन्द्रधनुष की पुनर्प्राप्ति के लिए लिखता हूँ,जिसे विकृत कर दिये जाने का ख़तरा है।''
हमें भी जनता के साहित्य और जनता के साहित्यकारों की शानदार परम्परा को विस्मृत कर दिये जाने के विरुद्ध लड़ना होगा। हमें लिखने को लड़ने का अंग बनाना होगा और इसमें निहित सारी परेशानियाँ,सारे जोखिम उठाने होंगे। मुक्ति स्वप्नों के इन्द्रधनुष को विस्मृति में खोने से भी बचाना होगा और विकृतिकरण की कोशिशों से भी। सृजन-कर्म की एकमात्र यही सार्थकता हो सकती है।
↧
विचारधारा का वर्गआधार
सत्ताधारी वर्ग के विचार हर युग में सत्ताधारी विचार हुआ करते हैं : अर्थात् जो वर्ग समाज की सत्ताधारी भौतिक शक्ति होता है,वह साथ ही उसकी सत्ताधारी बौद्धिक शक्ति भी होता है। जिस वर्ग के पास भौतिक उत्पादन के साधन होते हैं,उसका साथ ही साथ बौद्धिक उत्पादन पर भी नियंत्रण रहता है,और इस तरह साधारणतया जिन लोगों के पास बौद्धिक उत्पादन के साधन नहीं होते,उनके विचार इस वर्ग के अधीन रखे जाते हैं। सत्ताधारी विचार प्रभुत्वशाली भौतिक सम्बन्धों की,यानी विचारों के रूप में ग्रहण किये जाने वाले भौतिक सम्बन्धों की बौद्धिक अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं होते;अत: वे उन सम्बन्धों की अभिव्यक्ति हैं,जो एक वर्ग को सत्ताधारी बनाते है;इसलिए वे उसके प्रभुत्व के विचार हुआ करते हैं। जिन लोगों को लेकर सत्तारूढ़ वर्ग बनता है,उनके पास अन्य बातों के अलावा चेतना होती है,इसलिए वे सोचते हैं। इसलिए वे जहाँ तक एक वर्ग के रूप में शासन करते हैं तथा एक युग का विस्तार तथा परिधि निर्धारित करते हैं,उस हद तक यह स्वत: स्पष्ट है कि वे यह कार्य इसके पूरे फैलाव के साथ करते हैं,इसलिए अन्य बातों के साथ चिन्तकों के,विचारों को पैदा करने वालोंके रूप में भी शासन करते हैं और अपने युग के विचारों की रचना तथा वितरण का नियमन करते हैं: इस प्रकार उनके विचार युग के सत्ताधारी विचार होते हैं। उदाहरण के लिए,ऐसे युग में तथा ऐसे देश में,जहाँ शाही सत्ता,अभिजात वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग आधिपत्यके लिए होड़ कर रहे हों और इस कारण आधिपत्य विभक्त हो,वहाँ सत्ता के विभाजन का सिद्धान्त प्रभुत्वपूर्ण विचार सिद्ध होता है तथा ''चिरन्तन नियम''के रूप में अभिव्यक्त होता है।
श्रम विभाजन,जैसा कि हम उसे ऊपर (पृष्ठ [30-33])अब तक इतिहास की प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में देख चुके हैं,सत्ताधारी वर्ग में भी मानसिक तथा भौतिक श्रम के विभाजन के रूप में अपने को प्रकट करता है,इस तरह इस वर्ग के अन्दर एक भाग वर्ग के चिन्तकों (उसके सक्रिय,विचारक्षम सिद्धान्तकारों जो अपने बारे में इस वर्ग के भ्रमों को सर्वांगपूर्ण बनाने के काम को अपनी आजीविका का मुख्य साधन बनाते हैं) के रूप में प्रकट होता है,जबकि दूसरे लोग इन विचारों और भ्रमों के प्रति अधिक निष्क्रिय होते हैं,वे इन्हें सिर्फ आत्मसात् ही कर सकते हैं,क्योंकि वे ही वस्तुत: इस वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं तथा उनके पास अपने बारे में भ्रम तथा विचार संवारने के लिए कम समय होता है। इस वर्ग के अन्दर यह विभाजन दोनों भागों के बीच एक हद तक विरोध तथा वैरभाव में भी बदल सकता है,परन्तु वह व्यावहारिक टकराव की दशा में,जिसमें स्वयं वर्ग का अस्तित्व ही ख़तरे में पड़ सकता है,अपने आप खत्म हो जाता है,उस दशा में यह दिखावा भी लुप्त हो जाता है कि सत्ताधारी विचार सत्ताधारी वर्ग के विचार नहीं थे और उनमें इस वर्ग की शक्ति से अलग शक्ति थी। किसी काल विशेष में क्रांतिकारी विचारों का अस्तित्व एक क्रांतिकारी वर्ग के अस्तित्व का पूर्वानुमान करता है;इस क्रांतिकारी वर्ग के पूर्वाधारों के बारे में ऊपर काफी कुछ कहा जा चुका है(पृष्ठ [32-35])।
यदि हम अब इतिहास के गतिक्रम पर विचार करते समय सत्ताधारीवर्ग के विचारों को स्वयं सत्ताधारी वर्ग से पृथक् कर दें तथा उन्हें एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करें,यदि हम इन विचारों की रचना तथा उनके रचनाकारों की अवस्थाओं पर ग़ौर करने का कोई कष्ट किये बिना अपने को यह कहने तक सीमित रखें कि ये या वे विचार एक निश्चित काल में हावी थे,यदि हम इस प्रकार उन व्यक्तियों तथा अवस्थाओं को उपेक्षित करें,जो विचारों के स्रोत थे,तो हम,उदाहरण के लिए,कह सकते हैं कि उस काल में जब अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था,प्रतिष्ठा,निष्ठा आदि सम्प्रत्ययन तथा बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व के दौरान स्वतंत्रता,समानता,आदि सम्प्रत्ययन प्रभुत्वशाली थे। कुल मिलाकर स्वयं सत्तारूढ़ वर्ग इसे इसी तरह मानता है। इतिहास के इस सम्प्रत्ययन को,जो तमाम इतिहासकारों में विशेष रूप से अठारहवीं शताब्दी से व्याप्त है,आवश्यक रूप से इस घटना-दृश्य का सामना करना पड़ेगा कि अमूर्त विचार,अर्थात् वे विचार अधिकाधिक रूप से हावी हैं,जो अधिकाधिक रूप से सार्वत्रिकता का रूप ग्रहण करते हैं। बात यह है कि हर नया वर्ग,जो अपने से पहले शासन करने वाले वर्ग के स्थान पर अपने को प्रतिष्ठापित करता है,अपनी लक्ष्य सिद्धि की ख़ातिर ही अपने हित को समाज के तमाम सदस्यों के समान हित के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है,यानी,यदि हम विविक्त विचारणा के रूप में कहें,तो उसे अपने विचारों को सार्वत्रिकता का रूप देना पड़ता है और उन्हें एकमात्र युक्तियुक्त,सार्वत्रिक रूप से वैध विचारों के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। क्रांति करने वाला वर्ग - यदि और कारण नहीं,तो इसी कारण कि वह दूसरे वर्ग के विरुद्ध है - आरम्भ से ही एक वर्ग के रूप में नहीं,वरन् पूरे के पूरे समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होता है;वह एक सत्ताधारी वर्ग के खि़लाफ़ खड़े समाज के पूरे जनसमूह के रूप में प्रकट होता है।*वह ऐसा इसलिए कर सकता है कि आरम्भ में उसका हित सचमुच तमाम अन्य गैर सत्ताधारी वर्गों के समान हित से जुड़ा होता है,क्योंकि अबतक विद्यमान अवस्थाओं के दबाव के अन्तर्गत उसका हित अभी विशेष वर्ग के विशेष हित के रूप में विकसित नहीं हो पाया। अतएव उसकी विजय अन्य वर्गों के,जिन्हें प्रभुत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं होती,दूसरे बहुत लोगों को भी लाभ पहुँचाती है,परन्तु उसी हद तक लाभ पहुँचाती है,जिस हद तक वह अब इन लोगों को अपने को ऊपर उठाकर सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश करने की स्थिति में पहुँचाती है। फ्रांसीसी बुर्जुआ वर्ग ने जब अभिजात वर्ग की सत्ता उलटी,तो उसने इस तरह बहुत से सर्वहारा लोगोंके लिए अपने को सर्वहाराओं के ऊपर उठाना सम्भव बनाया,परन्तु सिर्फ उस हद तक,जिस हद तक वे बुर्जुआ बने। इसलिए हर नया वर्ग पहले शासन करने वाले वर्ग की तुलना में व्यापकतर स्तर पर ही अपना अधिनायकत्व हासिल करता है,जबकि नये सत्ताधारी वर्ग के विरुद्ध ग़ैर सत्ताधारी वर्ग का विरोध आगे चलकर और भी तीक्ष्णता तथा गहनता के साथ विकसित होता है। ये दोनों बातें यह तथ्य निर्धारित करती हैं कि इस नये वर्ग के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष,अपनी बारी में,तमाम पूर्ववर्ती वर्गों की अपेक्षा,जिन्होंने शासन हासिल किया था,समाज की पूर्ववर्ती अवस्थाओं के अधिक निश्चित तथा मूलगामी अस्वीकरण को लक्ष्य बनाता है।
अमुक वर्ग का शासन कतिपय विचारों का शासन मात्र है,इस सारे भ्रम का निस्सन्देह उस समय स्वाभाविक अन्त हो जाता है,जब वर्ग-शासन आम तौर पर समाज के संगठन के रूप में खत्म हो जाता है,अर्थात् ज्योंही किसी विशेष हित को सामान्य हित के अथवा ''सामान्य हित''को सत्ताधारी हित के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं रह जाता।
-कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स(ज़र्मन विचारधारा, 1846)
____________________________
*[हाशिये पर मार्क्स की टिप्पणी:] (सार्वत्रिकता इनके समरूप होती है:1) वर्ग बनाम श्रेणी ,2)प्रतियोगिता,विश्वव्यापी संसर्ग आदि,3) सत्ताधारी वर्ग की बहुत बड़ी संख्यागत शक्ति, 4) समानहितों की भ्रान्ति;आरम्भ में भ्रान्ति सही होती है, 5) सिद्धान्तकारों के भ्रम तथा श्रम-विभाजन।
↧










